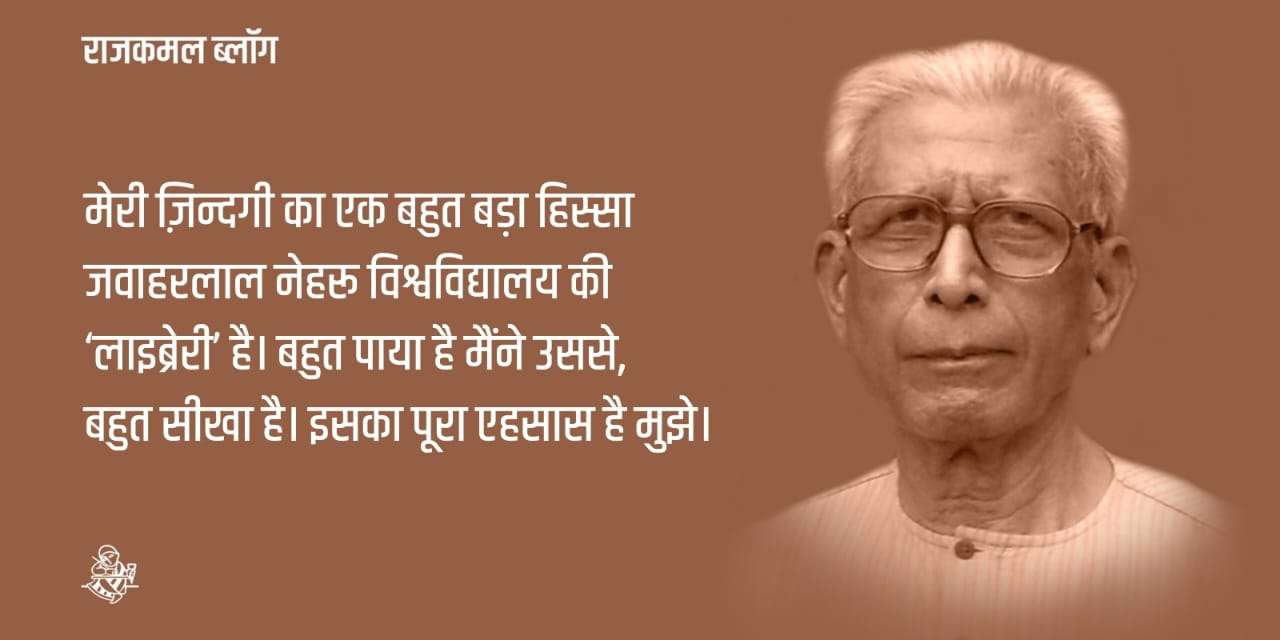
नामवर सिंह की जयंती पर राजकमल ब्लॉग में पढ़ें, सुमन केशरी द्वारा सम्पादित किताब ‘जेएनयू में नामवर सिंह’ का एक अंश जिसमें नामवर सिंह ने जेएनयू में भारतीय भाषा विभाग की शुरूआत से जुड़ें कुछ संस्मरण साझा किए हैं।
***
...तब हिन्दी-उर्दू के हम सिर्फ चार अध्यापक थे और छात्र भी छह, वे भी हिन्दी के। एक नया सेन्टर इसी पूँजी से शुरू हुआ था। आज उस सेन्टर में हिन्दी-उर्दू के बारह अध्यापक हैं। छात्रों की संख्या भी साठ से ऊपर ही होगी। आँकड़े के हिसाब से यह तीन गुनी बल्कि और ज्यादा तरक्की कही जाएगी। लेकिन जो सपना था, जो विज़न था उसको देखते हुए शायद यह बहुत सन्तोषप्रद न हो। प्रो. अनिल भट्टी को स्मरण होगा और प्रो. प्रमोद तालगिरी को भी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में आने से पहले ‘स्कूल ऑफ लैंग्वेजेज’ की ओर से एक सेमिनार किया गया था। उस सेमिनार की चर्चा का मुख्य विषय था कि भारतीय भाषाओं का जो सेन्टर बनेगा या बनना चाहिए उसका रूप क्या होगा? और मुझे उसमें भाग लेने के लिए जोधपुर से बुलाया गया था। उस सेमिनार ने मेरे सामने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का जो रूप रखा वह मेरे लिए एक आकर्षण और चुनौती की चीज थी। इन अठारह वर्षों में जो कुछ किया, जो कुछ हुआ, जो कुछ लिखा; उसमें साल भर की सबेटिकल छुट्टी के दौरान लिखी हुई ‘दूसरी परम्परा की खोज’ मेरे लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उस किताब के लिए मैं विश्वविद्यालय का ऋणी हूँ।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आने से पहले ‘मुक्तिबोध’ की चार पंक्तियाँ मेरे दिमाग में बराबर गूँजती रहती थीं। आज भी मेरे साथ हैं और आगे भी रहेंगी। और वह सवाल था कि “अब तक क्या किया/जीवन क्या जिया/ज्यादा लिया और दिया बहुत-बहुत कम/मर गया देश, अरे, जीवित रह गए तुम!!” यह एक चुनौती थी। हमने इस समाज से, इस देश से कितना लिया है! आज इनसान से एक दर्जा नीचे रहनेवालों की तादाद हमारे देश में नब्बे फीसदी से ज्यादा है। हम अध्यापक और विद्यार्थी उनकी तुलना में कितनी सुविधाओं से सम्पन्न हैं? एक ओर यह सब कुछ तो देश की जनता से ही मिला है, पैसा मिला है, सारी सुविधाएँ मिली हैं। उसकी तुलना में अगर हम देखें तो हमने क्या दिया है उन लोगों को? यह मेरे मन में बार-बार सवाल उमड़ता था और चूँकि हमारा साधन, हमारा माध्यम साहित्य है और साहित्य में भी जिसके बारे में हम कुछ थोड़ा-सा जानते हैं, वह एक भाषा का साहित्य है। उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? ये कुछ सपने थे, कुछ बेचैनियाँ थीं हमारे मन में, जिन्हें लेकर, जिनके लिए एक सही जगह की तलाश थी मेरे मन में। सच पूछें तो ख्याल थे कुछ, कुछ आइडियाज़ थे और उस नाटककार या उस ‘एक्टर’ की तरह से मुझे ‘थियेटर’ की तलाश थी, जहाँ मैं कम-से-कम वो ‘थियेटर ऑफ आइडियाज़’ कह लीजिए, ‘व्यूज’ कह लीजिए जहाँ मैं उस रंगमंच को भरे-पूरे रूप में प्राप्त करके कुछ कर दिखाऊँ। ज़ाहिर है, उसके लिए सहयोगियों की ज़रूरत थी और ऐसे कुछ सहयोगी मिले भी। एक ऐसा थियेटर भी मिला जो विचारों में उन्मुक्त था, खुला हुआ था, मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वह सब मिला। यह कुँवारी धरती थी, हर तरह से कुँवारी थी। मैं तो चार साल बाद आया। पर वे भाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने सन् 1970 से इस जमीन को तोड़कर यहाँ एक नई दुनिया बनाने की कोशिश की थी। लेकिन देखते-देखते... मुझे... अगर एक पोढ़ी-पकी, बनी-बनाई हुई यूनिवर्सिटी मिली होती तो शायद मैं या हम लोग वह नहीं कर पाते जो कर सके। इसलिए हमने तो कोरी पटिया से शुरू की। कोरी स्लेट से शुरू किया था और एक हद तक यह हमारे लिए सौभाग्य की बात थी और विश्वविद्यालय भी ऐसा मिला जो लगभग एक ‘लीजेंड’ उस समय बना हुआ था। धीरे-धीरे वह ‘लीजेंड’ अब तो टूट रहा है।
उस नए दौर में आने पर, इस नई दुनिया में आने पर मेरे भीतर एक नया इनसान बना और पैदा हुआ, जिसका एहसास इन अठारह वर्षों में तो नहीं हुआ, लेकिन अब इस विश्वविद्यालय को छोड़ते हुए महसूस करता हूँ। यहाँ विद्यार्थियों से, छात्रों से जो बौद्धिक चुनौतियाँ मिलीं, अगर वे नहीं मिलतीं तो हम लोग भी उसी तरह से एक खास तरह की ‘स्मॅगनेस’ के शिकार हो गए होते। रोजमर्रा जो चुनौतियाँ हमें विद्यार्थियों से कक्षाओं के बाहर होस्टल में, सड़कों पर, सेमिनार में मिलीं और उसके साथ ही मैं बहुत भाग्यशाली हूँ... किसी दूसरे विश्वविद्यालय में शायद वह अवसर न मिलता जहाँ मुझसे बेहतर, मुझसे ज्यादा अच्छे दूसरे शास्त्रों में, दूसरी विधाओं में, चाहे वह सामाजिक विज्ञान हो चाहे वह अन्तर्राष्ट्रीय विद्या संस्थान हो या विज्ञान के लोग हों, उन लोगों से मिलने, जानने और सीखने का मुझे अवसर मिला। एक ऐसी ‘लाइब्रेरी’ मिली और उस दौर के एक ऐसे ‘लाइब्रेरियन’ मिले... मेरी ज़िन्दगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की ‘लाइब्रेरी’ है। अगर कोई हाजिरी की किताब रहती तो पता चलता कि वहाँ जानेवालों में शायद सबसे नियमित यही आदमी था। कभी-कभी उन घड़ियों में भी, जब जानेवाले थोड़े लोग होते थे। बहुत पाया है मैंने उससे, बहुत सीखा है। इसका पूरा एहसास है मुझे। बाहरी आचार-विचार को देखनेवाले लोग नहीं जानते कि किसी आदमी के शरीर के अन्दर दौड़नेवाली वो हजारों नसें हैं, जो खून और खुराक पहुँचाती हैं। वो अदृश्य दान इस विश्वविद्यालय का मेरे लिए रहा है। कहीं पढ़ा था कि दत्तात्रेय के चौबीस गुरु थे। चौबीस तो खैर कहने के लिए थे। मशहूर यह था कि वे जहाँ भी जाते, वहाँ कुछ-न-कुछ सीखने के लिए मिल जाता। जैसे ओखली में मूसर चलानेवाली, धान कूटनेवाली औरत हो और उसकी चूड़ी झनझना रही हो, तो उससे भी दत्तात्रेय को कोई एक ज्ञान मिल जाया करता था। ऐसा जिज्ञासु होने का दावा तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैंने कोशिश की है कि यहाँ के प्रवास में जितने लोगों से सम्भव है, ज्ञान बटोर लूँ। वह बटोरी हुई पूँजी इस कदर मेरे मानस का हिस्सा बन चुकी है कि उसके मूल स्रोतों के नाम भी आज याद नहीं रहे।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आया तो हिन्दी सुनाई नहीं पड़ती थी। हिन्दी बोलनेवाले लड़के थे लेकिन उन्हें संकोच होता था। एक खास तरह की आधुनिकता थी। उसे मैं अंग्रेजियत नहीं कहूँगा। उसमें कुछ ‘बोहेमियन’ तत्त्व मिला हुआ था। लेकिन जिसे कहें कि एक गरीबी का भी गर्व हुआ करता है, एक गँवारपन का भी स्वाभिमान हुआ करता है, उस स्वाभिमान के साथ इस पूरे विश्वविद्यालय में यह गँवार आदमी धोती-कुर्ता पहने हुए खड़ा रह सका। यह ताकत मुझे अपने गाँव के लोगों से, बनारस से मिली थी। मुझे लगता था कि यह देसीपन इस विश्वविद्यालय के लिए बहुत ज़रूरी है। ये विश्वविद्यालय उस विदेशी हवा-पानी के खुराक से जवाहरलाल नेहरू के नाम को सार्थक नहीं कर पाएगा। ये देसीपन अपने आप इस विश्वविद्यालय में जुड़कर एक नई ताकत, एक नई शक्ति बना। जो मुझे बल देता रहा है। मित्रों ने जिक्र किया कि हिन्दी की जो ‘स्टीरियो टाइप’ एक तस्वीर बनी थी, उसे मैं तोड़ना चाहता था और उस तस्वीर को तोड़ने के लिए ज़रूरी था कि हिन्दी केवल अपनी पहचान अकेले दम पर, केवल हिन्दी को लेकर नहीं बना सकती। इसके लिए सगी बहन उर्दू का साथ जरूरी है। स्कूल बोर्ड की अपनी पहली बैठक में सेन्टर का पाठ्यक्रम प्रस्तुत करते हुए मैंने प्रस्तावना के रूप में कहा था और विश्वविद्यालयों में उर्दू और हिन्दी के विभाग जो जी चाहे करें, हम तो जेएनयू में, हमारा सेन्टर ऐसा बने जहाँ कि गंगा जमुनी संगम चाहते हैं। बड़ा फर्क पड़ेगा इससे। प्रस्ताव का स्वागत करनेवालों में एन. के. वी. मूर्ति पहले सदस्य थे, जो इस विश्वविद्यालय के प्रथम रजिस्ट्रार रह चुके थे। और अब भी यह अकेला विश्वविद्यालय है जहाँ हिन्दी के विद्यार्थी को उर्दू पढ़ना और उर्दू के विद्यार्थी को हिन्दी पढ़ना अनिवार्य है। दूसरे विश्वविद्यालयों में जहाँ दोनों भाषाएँ पढ़ाने और पढ़नेवाले एक-दूसरे से लड़ने के लिए बदनाम हैं, हमारे छात्रों ने, हमारे सहयोगियों ने दोस्ती की एक मिसाल पेश की है।... प्रेमचन्द के ‘गोदान’ उपन्यास में होरी की आखिरी बात याद आती है। होरी कहता है, “जो कुछ अपने से नहीं बन पड़ा उसी के दुखों का नाम तो मोह है। पाले हुए कर्तव्यों और निपटाए हुए कामों का क्या मोह! मोह तो उन्हें छोड़ जाने का है जिनके साथ हम अपना कर्तव्य निभा नहीं सके, उन अधूरे मनसूबों में है, जिन्हें हम पूरा नहीं कर सके।”
इस क्षण जबकि हर तरह के मोह से आदमी को मुक्त होना चाहिए, अजीब बात है कि इनसान होने के नाते उस मोह से, जो अधूरे मनसूबे हैं, उनसे मुक्त होना बड़ा कठिन लगता है। एक सपना था कि हिन्दी-उर्दू के साथ कम-से-कम दक्षिण की एक भाषा हो, पश्चिम की एक भाषा हो, पूरब की एक भाषा हो और आधार रूप में संस्कृत हो। इन्हें मिलाकर कम-से-कम एक ऐसे भारतीय साहित्य, तुलनात्मक साहित्य की तस्वीर रखी जाए, जहाँ हर भाषा अपनी पहचान कायम रखते हुए भारतीय साहित्य की व्यापकता का आभास दे। फिर, ‘स्कूल ऑफ लैंग्वेजेज़’ से बड़ा विदेशी भाषाओं के अध्ययन का कोई संस्थान इस देश में नहीं है। रूसी, जर्मन, फ्रेंच, स्पैनिश, चीनी, जापानी के साथ ही अरबी, फ़ारसी इत्यादि भाषाओं की सर्वोच्च पढ़ाई यहीं होती है। ऐसे वातावरण में तुलनात्मक अनुशीलन की पद्धति अपनाकर भारतीय साहित्य क्या शक्ल ले सकता है, यह सोचते ही “तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुत हरे:। विस्मयो मे महान्यजन् हृष्यामिच पुन: पुन:।” रोमांच हो आता है इसकी कल्पना करके। यह सपना हमारा रहा है और मैं समझता हूँ कि सपना देखना छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि कभी-कभी सपना देखने का अधिकार भी छिन जाता है। तब हकीकत भी मुरझा जाती है और मर जाती है। मुझे उम्मीद है कि भारतीय भाषा केन्द्र आगे आनेवाले समय में, और विश्वविद्यालय का इस ओर ध्यान जाएगा, सही मायने में भारतीय भाषाओं के साहित्य का मरकज़ और केन्द्र बन सकेगा।
[नामवर सिंह की किताबें यहाँ से प्राप्त करें।]
