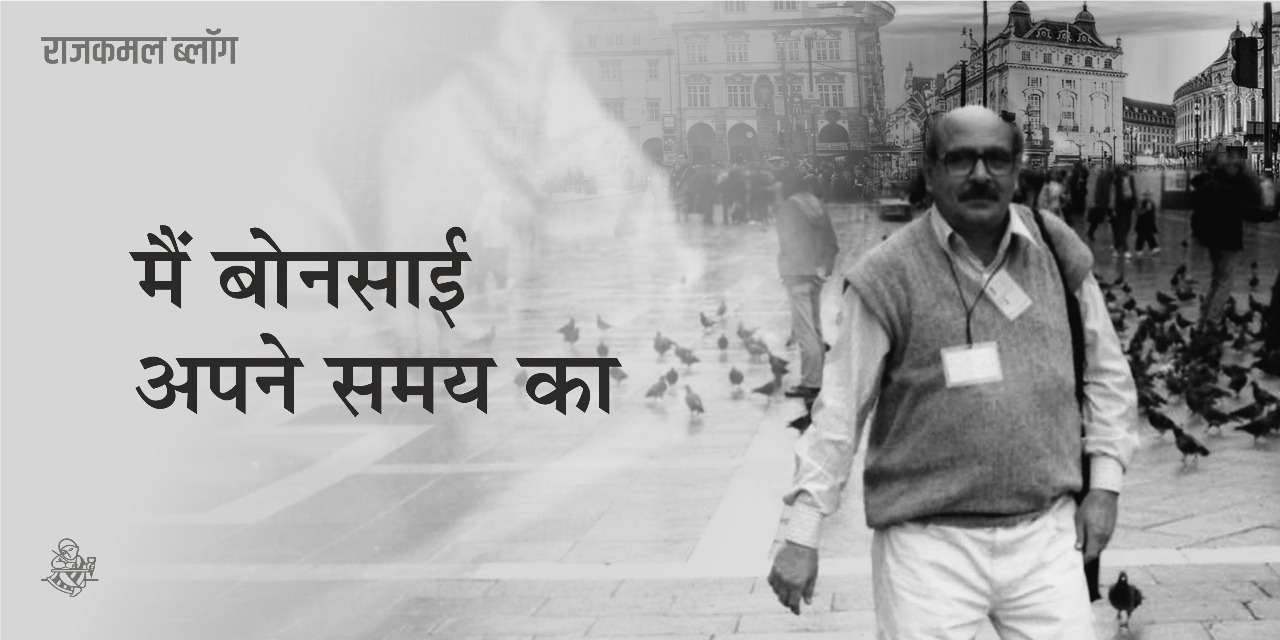
जानेमाने लेखक-पत्रकार रामशरण जोशी ने हाल ही में अपनी देह दिल्ली-एम्स को वैज्ञानिक शोध और प्रशिक्षण के लिए दान कर दी है। राजकमल प्रकाशन समूह समाजहित में लिए गए उनके इस फैसले का स्वागत करता है और उनका आभार व्यक्त करता है। हालांकि, देहदान करने की इच्छा वे अपनी आत्मकथा ‘मैं बोनसाई अपने समय का’ में कुछ वर्ष पहले ही व्यक्त कर चुके हैं। राजकमल ब्लॉग में पढ़ें, उनकी आत्मकथा का एक अंश।
***
दिसम्बर, 2013 में मैंने 32 क्रिस्ट रोड में जीवनकथा का अन्त से आरम्भ किया था। तब मैं सत्तर पार था। आज मैं तिहतर-प्रवेश की दहलीज पर खड़ा हूँ। दूसरे शब्दों में ‘अन्त का समापन’ लिख रहा हूँ—105 समाचार एपार्टमेन्ट्स में बैठ कर।
आज इस फ्लैट में आए करीब ढाई दशक गुजर चुके हैं। जंगपुरा एक्सटेंशन से उठकर जब पाँच सदस्यों का यह जोशी परिवार इस सीमेंट के घोंसले में आया था, तब यमुनाजी का पाट दिखाई दिया करता था। दूर-दूर तक हरियाली की चादर बिछी हुई थी। मैं अपनी बालकनी और छत से हुमायूँ मक़बरा, लोट्स टैम्पल, नेहरू स्टेडियम, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन के बुर्ज आदि सब कुछ देख सकता था।
घर से राष्ट्र के सत्ता पुंज साउथ ब्लॉक का फ़ासला तेरह-चौदह किलोमीटर है। पर, तब आसमान साफ़ रहता था। नील गगन की छाँव कितनी पारदर्शी हुआ करती थी। तब न कोई अक्षरधाम था, न ही राष्ट्रमंडल खेलों का स्टेडियम व एपार्टमेन्ट्स और न ही फ्लाई ओवर! तब ‘राष्ट्रमंडल खेल घोटाला’ भी कहाँ था?
आज मेरी बालकनी के सामने से मैट्रो ट्रेनें धड़ाधड़ गुजर रही हैं। पहले जो थोड़ा-बहुत शहरी वन क्षेत्र हुआ करता था, वह लुप्त हो चुका है। उसकी क़ब्र पर मैट्रोलाइन बिछा दी गई है मीलों लम्बी। हमारी ‘स्काई लाइन’ को हाईटेंशन तारों, फ्लाई ओवरों के रैम्प पर फैशन परेड करती रंग-बिरंगी कारों ने ढाप दिया है। एक तेज रफ्तारी सभ्यता मंथर गतिवाली सभ्यता की छाती पर पसर गई है। अब जोशी परिवार इसका बरबस नागरिक है, एक सभ्यता का अन्त है, दूसरी का उदय है!
शायद जीवन की कथा भी इससे भिन्न नहीं है। किसी भी कथा का न अन्त है और न आरम्भ। व्यक्ति अपनी सुविधा और ज्ञान-क्षमता से इसे आरम्भ व अन्त या अन्त व आरम्भ में विभाजित करता रहता है। मैंने भी कुछ-कुछ ऐसा ही किया है। इसकी वजह है, क्योंकि सब कुछ अनिश्चित है। जीवन-यात्रा का एक रोज निश्चित ही पटाक्षेप होगा। लेकिन यह पर्दा किस रोज, कहाँ और कैसे गिरेगा, यह तो मुअय्यन नहीं है न! तब आरम्भ और अन्त की विभाजक तारीख़ या ‘कट ऑफ डेट’ कैसे निर्धारित व परिभाषित की जाए? यह प्रश्न तो अनुत्तरित या पहेली ही रहा न मेरे लिए! अलबत्ता, इन दिनों भूकम्प के झटकों की फ्रीक्वेंसी (अप्रैल-मई, 15) बढ़ गई है। प्राकृतिक और राजनीतिक, दोनों ही क्षेत्रों में!
मध्यमवर्ग का सदस्य होने के नाते सोच लिया था सत्तर-पचहत्तर बरस जी लेंगे। इससे ज्यादा उम्र क्या होगी! सो, इस बंदे ने उसी हिसाब से परिवार के गैस-बर्नर को जलाये रखने के लिए पन्द्रह-बीस हजार रुपए महीने का बंदोबस्त कर लिया था। बैंक में एफडी जमा करायी और पोस्ट ऑफिस में मासिक बचत खाता खोला। तब कहाँ सोचा था कि मोहन-मोदी मार्का राजनीतिक अर्थव्यवस्था की बदौलत कमरतोड़ महँगाई होगी, डॉलर के सामने रुपया मरियल बनने लगेगा, डेढ़-डेढ़ लाख करोड़ रुपए के घोटालों की बरसात होगी, बैंकों की ब्याज दर घटेगी, राज्य दल्ला (फेसीलिटेटर) का रोल अदा करने लगेगा और कॉरपोरेट घरानों पर बहार उतरेगी!
अपने राम तो मस्त थे कि भारत ‘लेफ्ट टू दी सेंटर’ की पटरी पर चलता रहेगा। आज तो लेफ्ट ही पटरी से उतर कर पगडंडी पर आ चुका है! तब यह मध्यवर्गीय नागरिक क्या करे! कोई पेंशन तो है नहीं, एफडी की ब्याज दर घटती जा रही है। तब क्या इस परिदृश्य में एक स्वाभिमानी व्यक्ति अपनी जीवन-यात्रा पर विराम लगा दे? आत्महंता किसानों का अुनयायी बन जाए?
यह प्रश्न, यह विचार किसी को भी आतंकित कर सकता है। वास्तव में, आज स्वाभिमान और गरिमा के साथ जीना प्रतिदिन दूभर होता जा रहा है। विकल्प सूखते-सिकुड़ते जा रहे हैं। देश के तथाकथित ‘कलश’ राष्ट्र के बोनसाईकरण के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं।
ऐसे दौर में मुझे ‘मेरा बंधु’ कहानी बरबस याद आ रही है। 2004 में ज्ञानरंजन जी ने अपनी प्रसिद्ध पत्रिका ‘पहल’ के 76वें अंक में मेरी इस कहानी को प्रकाशित किया था। हालाँकि मैं कहानीकार नहीं हूँ। लेकिन समय के उद्वेगों ने मुझ से यह प्रयोगात्मक कहानी लिखवायी थी। यह टफ व अमूर्त कहानी है जिसमें राष्ट्र की अन्तरात्मा के बोनसाईकरण व आत्मसमर्पण की प्रक्रिया का चित्रण है। ज्ञान जी ने इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया था। ज्ञान जी के सम्पादकीय विवेक पर तो सवालिया निशान नहीं लगाया जा सकता। फिर भी आत्मग्रस्त हिन्दी के लेखक समाज की ख़ामोशी को अबूझ पहेली ही कहा जाएगा।
एक रोज तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के यहाँ आयोजित कलेवा-अवसर पर अशोक वाजपेयी जी ने हैरत से इतना जरूर पूछा था, क्या ‘पहल’ में प्रकाशित ‘मेरा बंधु’ कहानी के आप ही लेखक हैं? फिलहाल तो मैं ही हूँ, अशोक जी! मैंने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया था। अशोक जी के शब्दों ने भोपाल के ‘आग्नेय सिंड्रोम’ को पुनर्जीवित कर दिया था। आज यह सिंड्रोम ढह चुका है, मैं यक़ीन के साथ नहीं कह सकता। यह अलग बात है कि मेरे पत्रकार मित्र और अशोक-मंडली के ही अन्तरंग सदस्य ओम थानवी ने दस वर्ष पश्चात् मार्च, 2014 में ‘मेरा बंधु’ पर टिप्पणी की थी, कहानी लाजवाब है। कसी हुई और बेलौस है।
फिर भी मैं कितने और बसंत-पतझर का सहयात्री बनूँगा, यह प्रश्न मुझे निरंतर छकाता रहता है। कभी-कभी तीव्र इच्छा होती है कि यह निरीश्वरवादी कुछ पलों के लिए ‘आस्तिक’ बन कर उससे कहे, मुझे इस भूलोक को शान्तिपूर्वक अलविदा कहने दे, एक हिचकी के साथ ही अनन्त-अनाम-अज्ञात में मैं विलीन हो जाऊँ, क्योंकि मेरा गणित साफ़ है—अस्पतालों में भर्ती होने का अर्थ है तमाम जमापूँजी का चंद दिनों में स्वाहा हो जाना! इसके पश्चात् स्वतंत्रता की इति और बच्चों पर आश्रित होना। बड़ा तकलीफ़देह होगा वह दिन!
दयनीयता-अस्सहायता मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु होती है। यह स्थिति नरक समान होती है। मैं इससे बचना चाहता हूँ। मैं अपने पिता की भाँति एक ही पल में जैव से अजैव में रूपांतरण चाहता हूँ। मैं स्वार्थी हो रहा हूँ न! यह ‘मोहन-मोदी स्पेशल इफेक्ट्स’ हैं; इसे न मैं बदल पा रहा हूँ, और न ही इससे पलायन कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ, जब रक्त-मांस का यह चलता-फिरता पिंड अजैव पदार्थ में रूपांतरित हो जाए तो इसे किसी सरकारी अस्पताल या मेडिकल कॉलेज को सुपुर्द कर दिया जाना चाहिए, ताकि कहीं, किसी के लिए यह अपनी अंतिम अकिंचित् भूमिका निभा सके!
मैं सभी भूमिकाएँ निभा चुका हूँ, सिवाय एक को छोड़। भौतिक दृष्टि से मैं स्वयं को असफल नहीं कह सकता, कई उपलब्धियाँ हैं खाते में। पर मैं ‘फ्रस्टेशन’ से मुक्त हूँ, यह दावा करना ढकोसला कहलाएगा। मेरे जीवन का एकमात्र फ्रस्टेशन या कुंठा यही है कि मैं क्रान्तिकारी नहीं रह सका, क्रान्ति नहीं कर सका, क्रान्ति-पथ से पलायन किया, भगोड़ा बन गया! मैंने मध्यवर्ग की नियति के (या स्वयं का बोनसाईकरण) के वरण के साथ ही स्वयं का पिण्डदान कर दिया! मैं ‘मेरा बंधु’ बन गया हूँ।
[रामशरण जोशी की पुस्तकें यहाँ से प्राप्त करें।]
