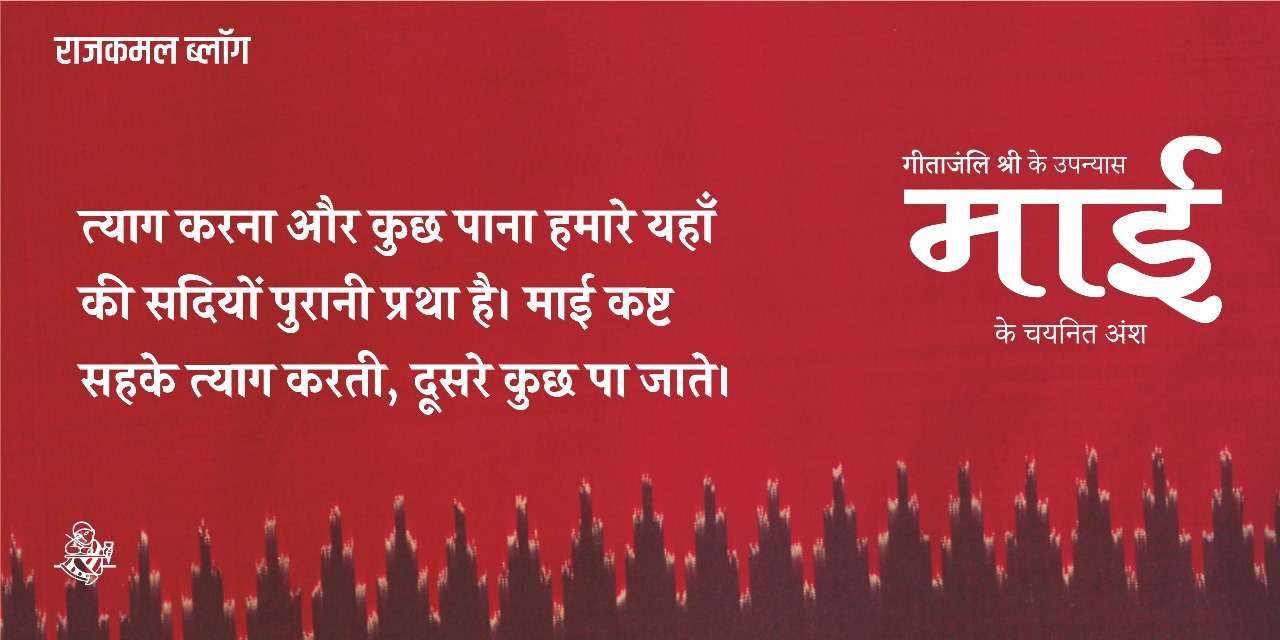
“माई में हम और माई हमारे लिए, यही हमारा जानना था। तभी उसका सबकी मंशापूर्ति के लिए कठपुतली बनना, फिर उनके जूठन पर ज़िन्दा रह लेना, हमें क्रोध से पागल किए जा रहा था। दादा को मकुनी और फुलौरा पसन्द तो वह उनका, जब किसी को नहीं चाहिए तो माई का; दादी को धुसका पसन्द तो वह उनका, बासी हो चले तो माई का। बाबू जो छोड़ें वह माई का। हमें जो पसन्द वह चुपचाप माई को नापसन्द। दादा-दादी को तो फ्रिज का खाना भी नापसन्द-ताज़ा के बाद खाना तामसी हो जाता है, दादी कहतीं तो वह सारा माई का।”
राजकमल ब्लॉग में पढ़ें, बुकर पुरस्कार से सम्मानित लेखक गीताजंलि श्री के पहले उपन्यास ‘माई’ के कुछ खास अंश। पहली रचना से ही लेखक को साहित्यिक समाज के बीच चर्चा का केन्द्र बनाने वाले इस उपन्यास में एक छोटे शहर की बड़ी-सी ड्योढ़ी में बसे एक परिवार की कहानी है। जिसमें एक मध्यमवर्गीय परिवार में औरत की ज़िन्दगी को बड़े प्रभावशाली तरीके से उभारा गया है।
...
माई कब उठती थी, क्या खाती थी, कैसे रहती थी, शुरू में तो हमने सोचा ही नहीं। और बाद में जब सोचने लगे तो हम उसको चाहते और उस पर दया करते। [पृ.सं. 17]
***
माई का पर्दा देखकर हमें उसके पीछे का खयाल ही न आया। माई की सहनशीलता और लाज का प्रशान्त वह पर्दा। सबकी सुनती, सबकी करती वह सीरत-पाक छाँह। [पृ.सं. 22]
***
हमने माई को डाँटा था क्यों तुम दादी को इतना सब कहने देती हो। माई ने बताया था वह जो दादी के सिर पर एक जगह बाल उड़े हैं, बुढ़ापे की देन नहीं है। जो भीतर वह बक्सों का कमरा है दादी वहाँ घुस जाती थीं और दादा नशे में उसे खींचते थे। माई ने कहा था दादी और उसकी जात एक है, हमजात को वह ठुकरा नहीं सकती। और मैं अपने रूप में उन दोनों की छवि पाकर एक अजीब-सी कमज़ोरी महसूस करती हूँ। कोस नहीं पाती उन्हें जिनकी शक्ल-सूरत मेरे चेहरे और बदन पर झलकती है। [पृ.सं. 36]
***
सभी को फ़िक्र रहती। बस माई को पता नहीं रहता, हम कुछ करें, कहीं हों। सब मुझे ‘असली पर्दे’ में बिठाने को बेक़रार, वह जैसे भूल से ही मेरा पर्दा ठीक से बँधने के पहले ही खिसका देती।
फिर भी वह तो अल्पसंख्यकों में थी, जब होता पर्दा हिला देती लेकिन बहुमत ऐसे कसके पकड़ने लगा कि पर्दा पूरी तरह हट नहीं पाता। मैं कुछ अन्दर, कुछ बाहर होते-होते शायद असली पर्दा करने ही लगी। आँखें झुकने लगीं, आवाज़ दब गई, कन्धे भी सिकुड़ने लगे...।
पर तब वह ‘लौ’ जो पर्दे के पीछे सुलग रही थी, पर्दे के बार-बार हिलने से हवा पाकर भड़क उठी और आग बनके पर्दे को ही जला बैठी।
यह आग माई की लगाई है, दादी कहतीं, सुबोध की करनी है, दादा कहते, और बाबू, दिल का दौरा न पड़े इस कोशिश में सीने पर हाथ मलते रहते ।
और माई ?
वह कुछ न कहती। वह तो पर्दा करती थी। उसके पर्दे में लौ सुलगी होगी तो उसे उसने बाहर न बढ़ा भीतर खींच लिया होगा।
यह भी तो एक फ़र्क था माई और मुझमें। उसकी आग अन्दर को गई, मेरी बाहर को निकली। जले तो होंगे दोनों ही...। [पृ.सं. 47-48]
***
अपने से अलग माई को कभी नहीं देखा। उसका जीवन ही, हमारा मानना था, हमारे बचपन से शुरू हुआ।
वह तो बाद में उसकी आँखों से झरी ठंडी राख मिली। और तब कितनी ही चीज़ों पर उस राख का कोई ज़र्रा पड़ा मिल गया।
माई में हम और माई हमारे लिए, यही हमारा जानना था। तभी उसका सबकी मंशापूर्ति के लिए कठपुतली बनना, फिर उनके जूठन पर ज़िन्दा रह लेना, हमें क्रोध से पागल किए जा रहा था। दादा को मकुनी और फुलौरा पसन्द तो वह उनका, जब किसी को नहीं चाहिए तो माई का; दादी को धुसका पसन्द तो वह उनका, बासी हो चले तो माई का। बाबू जो छोड़ें वह माई का। हमें जो पसन्द वह चुपचाप माई को नापसन्द। दादा-दादी को तो फ्रिज का खाना भी नापसन्द—ताज़ा के बाद खाना तामसी हो जाता है, दादी कहतीं तो वह सारा माई का। [पृ.सं. 49-50]
***
हम माई को बचाते रहे। वह कमज़ोर है, कठपुतली है, हमारे अलावा उसका कोई नहीं है। इतनी कमज़ोर है वह कि हम उसके लिए लड़ते हैं और वह ऐन वक़्त पर पीछे हट जाती है और हमारी चीख हवा से टकराकर चारों दिशाओं में छितर जाती। इस तरह-सुबोध ने नाटक के टिकट खरीदे, माई ने रेशमी साड़ी पहनी, बाबू ने निकलते निकलते टोक दिया— ‘तुम भी? क्या ज़रूरत?’ और माई रुक गई, सुबोध बकता रहा, माई ने साड़ी बदली, चौके में चली गई। [पृ.सं. 51]
***
त्याग करना और कुछ पाना हमारे यहाँ की सदियों पुरानी प्रथा है। माई कष्ट सहके त्याग करती, दूसरे कुछ पा जाते। व्रतों की ही लम्बी फेहरिस्त थी जो सारे के सारे वह रखती थी। कोई पति की मंगलकामना के लिए, कोई पुत्र के लिए, सन्तान के लिए। [पृ.सं. 53]
***
असर था। मुझ पर। माई का। पीढ़ियों की सारी माइयों का जिन्होंने दूसरों के लिए ‘सह’ कर, उन्हें सफलता दिलाके, वही अपनी सफलता जानी। जिनकी उन सहती हुई आहों का असर उस हवा में तिर गया जो मैंने अपनी साँसों में खींची। वे आहें जिन्हें मैं बार-बार साँस छोड़के बाहर निकाल देना चाहती पर बार-बार साँस लेके फिर भीतर खींच लेती। माई, जो हर ‘देने’ में थी, मुझमें भी आ गई। [पृ.सं. 63]
***
मैं माई नहीं बन पाऊँगी। वह सिफ़त ही इस सदी से लोप होती जा रही है। मैं माई बन भी सकती तो भी नहीं बनना चाहूँगी। मुझे माई नहीं बनना। जी-जान से लडूंगी कि माई नहीं बनूँ। ज़ोर से झकझोरकर अपने अन्दर से माई को झटका देना चाहती हूँ। हर तरह के ‘सहने’ को निकाल फेंकना चाहती हूँ। वह गलत है, मुझे वह रोकना है।
फिर भी मैं माई, जो मेरा आदर्श नहीं, जो वह है जिससे मैं लड़ती हूँ, जो वह है जो मुझे नहीं बनना, के आगे माथा टेक देती हूँ।
अपनी पिपासा में मैंने पंख फड़फड़ाए। माई नहीं बनना, कैदी नहीं बनना, सिकुड़कर नहीं रह जाना। [पृ.सं. 64]
***
माई ने आकाश में एक पंछी दिखाया था जो एक ही जगह तीव्र गति से उड़ने की प्रक्रिया में लीन था। ‘वह देखो।’ पंछी असीम अम्बर में एक ही जगह पंख फड़फड़ा रहा था। लग रहा था सारा आकाश उसी का है। [पृ.सं. 64]
***
आप ही झुक जाती हूँ, उस ‘अथाह कमज़ोरी’ के आगे जिसने मुझ ‘ताकतवर’ को आड़ दी। मेरी बेड़ियाँ खुलने दीं, आग लहकने दी, गति आने दी। उसकी अथाह कमज़ोरी ने ही मुझे लड़ा दिया। [पृ.सं. 64]
***
हमने तो जोड़ा तो बस माई को अपने आपसे जोड़ा। उसके खाली अन्तस में खुद को डाल दिया। उसके कमज़ोर डरपोक व्यक्तित्व में अपनी हिम्मत भरनी चाही।
होते-होते हम माई के साथ कुछ ऐसे हो गए जैसे पालतू कुत्ते होते हैं, पहरा देते होशियार खड़े! पहले जब हम डरते थे तो कोई उसे कुछ कहता, हम तड़ से नज़र ऊपर करते, आँखों में घबराहट और हमदर्दी लिये। फिर हम गुर्राने लगे। फिर वक़्त ज़रूरत भौंकने लगे। और करना पड़ता तो अगला कदम भी ले लेते—काटने का!
हम माई के लिए डरने लगे थे। उसे भी अपने साथ निकाल लेना चाहते थे। [पृ.सं. 83]
***
हम जानते थे वक़्त लगेगा, माई को दुनिया में चलना सीखने में वक़्त लगेगा। जब उसे खींच-खाँचकर बाहर ले आते तो माई नन्हीं-सी बच्ची बन जाती। हमारा हाथ पकड़कर सड़क पार करती, भीड़ में घबराई-सी घुसती। [पृ.सं. 99]
***
इसी बात का तो हमें बचपन से रंज था। “बोला करो माई, लड़ा करो, जो होना चाहती हो वह होओ।” इस तरह तो माई थी ही नहीं— झुकी, मूक, डरपोक छवि, जिसमें सिर्फ दूसरों के इशारों पे हरकत होती। हम दया से भर जाते। चिढ़ जाते।
और कोई था जिसे हम माफ़ नहीं कर पाते जिसने किसी को माई बनने दिया। क्योंकि माई ‘न बनने’ का पर्याय लगा। क्यों नहीं माई को असल, पूरा बनने दिया?
हम कभी ‘माई’ नहीं बनेंगे। मैं कभी ‘न बनी’ नहीं रहूँगी, यह घोर यक़ीन, इसी का गहरा संग्राम, यही हमारा जीवन था। [पृ.सं. 116]
[गीतांजलि श्री की पुस्तकें यहाँ से प्राप्त करें।]
