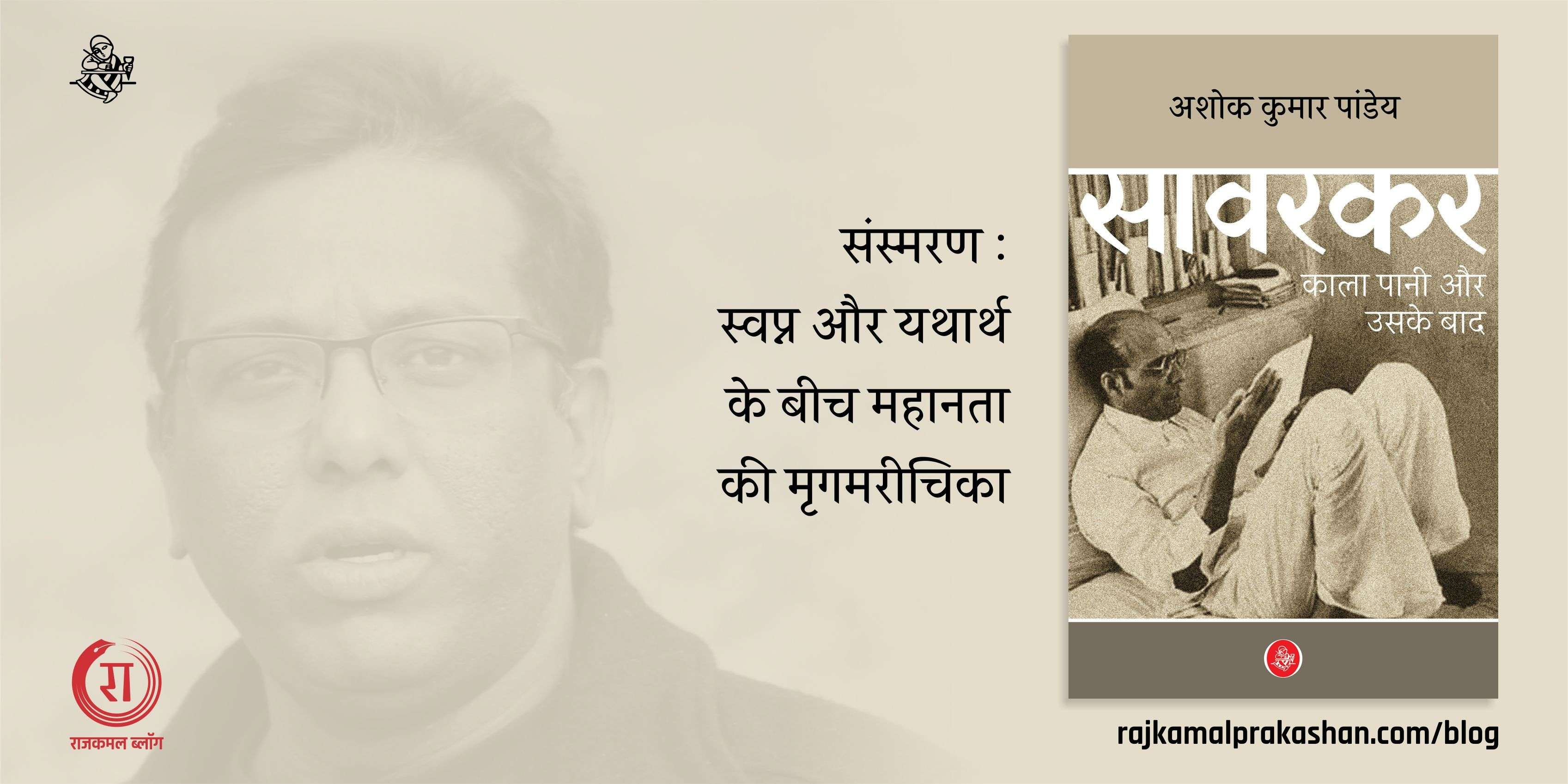
1939 में 'हरदयाल डे' पर दिए गए पूर्वोद्धृत भाषण में सावरकर प्रथम विश्वयुद्ध में ग़दर आन्दोलन के नेताओं के साथ खुद को जोड़कर ऐसे दर्शाते हैं मानो पूरे आन्दोलन का नेतृत्व वह खुद कर रहे थे। अपनी अतिरेकी तारीफ़ उनके लेखन की खासियत है, लेकिन 'धीरे-धीरे हमें जर्मनी से सम्बन्ध स्थापित करने में सफलता मिलने लगी' कहते हुए उन्हें एक क्षण के लिए भी क्या यह याद नहीं आया होगा कि इस विश्वयुद्ध के समय अंडमान की जेल से वह अपनी रिहाई के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हुए अंग्रेजी सरकार से इस युद्ध में सरकार द्वारा दी गई किसी भी भूमिका को निभाने का वादा कर रहे थे?" यही नहीं, अपने संस्मरण अंडमान की काल कोठरी से में सावरकर ने प्रथम विश्वयुद्ध को लेकर जो विचार व्यक्त किए हैं, वे ग़दर आन्दोलन से एकदम अलग हैं। जहाँ हरदयाल, वीरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय और राजा महेन्द्र प्रताप सिंह तुर्की के सहयोग से जर्मन तुर्की मिशन अफ़गानिस्तान भेजकर अंग्रेजी शासन का प्रतिकार खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं सावरकर अपने संस्मरण में लिखते हैं-
ग़ौर से पढ़ने पर साफ़ समझ आता है कि इस युद्ध में सावरकर अंग्रेज़ों के समर्थन और असल में अपने माफ़ीनामे को सही साबित करने की भूमिका बना रहे हैं। शिखंडी की तरह उन्हें इसके लिए मुस्लिम ख़तरे की आड़ लेनी पड़ रही है। सावरकर आगे लिखते हैं कि उनके संगठन ने कोई सशस्त्र संघर्ष की क़सम नहीं खाई है और 'देश को यदि उसकी अपनी प्रकृति के अनुसार तथा तत्सिथिति अनुसार स्वतंत्रता का उपभोग करने की अनुमति दी जाए तो उस साम्राज्य से एकनिष्ठ रहना हम अपना कर्तव्य समझेंगे।" उस दौर में औपनिवेशिक स्वायत्तता की यह माँग लगभग सभी राजनैतिक दल कर रहे थे तो यह उनसे अलग तो नहीं था, लेकिन जो सावरकर जेल में आने से पहले कांग्रेस, नौरोजी और यहाँ तक कि श्यामजी कृष्ण वर्मा के होम रूल लीग जैसी संवैधानिक लड़ाइयों का उपहास कर रहे थे, उनका जेल जाने के दो-तीन साल में ऐसा विचार परिवर्तन आश्चर्यजनक है, लेकिन आगे पढ़ने पर फिर समझ आ जाता है कि दरअसल यह ठकुरसुहाती की भूमिका है, माफ़ी के पहले का माहौल बनाना है। आगे वह लिखते हैं-
14 मई, 1939 के भाषण में 'इंग्लैंड का जो शत्रु वह हमारा मित्र है' यह भावना जाग्रत हुई कहने वाले सावरकर सितम्बर, 1914 को लिखे माफ़ीनामे में जर्मनी के खिलाफ़ इंग्लैंड की सेना में शामिल होने का प्रस्ताव दे चुके थे। दोनों ही बार मुसलमानों के कथित ख़तरे की आड़ में यह छल और प्रपंच करते हुए वह शर्मनाक से अधिक दयनीय नज़र आते हैं। अपनी ही गढ़ी हुई छवि में कैद लगातार झूठ बोलने पर विवश दयनीय व्यक्ति, जिसके कमज़ोर आत्मबल ने उसे एक प्रखर क्रान्तिकारी से एक दयनीय मिथ्यावादी में बदल दिया। उनके पास सुविधा बस यही थी कि उनके माफ़ीनामे गोपनीय दस्तावेजों में क़ैद थे। उस दौर में लोग यह नहीं जानते थे कि वह अंग्रेजों से क्या-क्या वादे करके छूटे हैं, किस-किस तरह माफ़ियाँ माँगी हैं क्योंकि ये माफ़ीनामे तो उनकी मृत्यु के बाद अस्सी के दशक में ही बाहर आ सके।
इस पूरे दौर में एक 'वीर' क्रान्तिकारी की तरह सम्मानित होने वाले सावरकर को यह डर तो रात-दिन सताता ही होगा कि कहीं वे गोपनीय दस्तावेज उनके जीते जी बाहर आ गए तो लोगों की नजर बदल जाएगी। इसी भय को उन्होंने नग्न साम्प्रदायिक प्रचार से ढका और साम्प्रदायिकता के नशे में डूबी एक ऐसी फ़ौज तैयार की, जिसके सम्मुख वह यह सिद्ध करने में सफल रहे कि शत्रु अंग्रेजी सरकार नहीं मुसलमान हैं। उन्हें भरोसा रहा होगा कि नफ़रत से भरी यह फ़ौज अंग्रेजी सरकार से उनके माफ़ीनामों और फिर सरकार के साथ सहयोग को 'हिन्दू हित' में किए कृत्य की तरह ही देखेगी, और उनका यह भरोसा सही साबित भी हुआ।
ख़ैर, उनके जेल जाने के बाद जब जुलाई, 1913 में ग़दर आन्दोलन शुरू हुआ तो वह अंग्रेज़ी सरकार को तीन माफ़ीनामे लिख चुके थे। ग़दर आन्दोलन और हरदयाल पर उनकी टिप्पणी उनके अपने मन की उपज है। असल में सावरकर के इस पूरे भाषण में ही तथ्यात्मक ग़लतियाँ हैं, जिन्हें सावरकर समग्र के हिन्दी सम्पादकों ने भी जाँचने की जरूरत महसूस नहीं की। जैसे सावरकर कहते हैं कि हरदयाल को अमेरिका ने गिरफ़्तार कर लिया, लेकिन जानबूझकर भागने दिया, जबकि तथ्य यह है कि उन्हें जमानत देते हुए अमेरिका छोड़ देने का आदेश दिया गया था। हरदयाल हथियार का रास्ता पूरी तरह छोड़कर शान्ति का प्रचार कर रहे थे और गांधी के प्रशंसक हो गए थे। सावरकर द्वारा हरदयाल की ग़रीबी और भारत आने के लिए भाई परमानन्द द्वारा पैसे देने की बात भी इस तथ्य के कारण सही नहीं लगती कि अपने जीवन के अन्तिम दौर में उन्होंने न केवल लन्दन यूनिवर्सिटी के 'स्कूल ऑफ़ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज' से पी-एच.डी. की डिग्री हासिल की थी और अपनी अन्तिम किताब हिंट्स ऑफ़ सेल्फ़ कल्चर' प्रकाशित करवाई थी, बल्कि योरप और अमेरिका में लगातार व्याख्यान भी दे रहे थे। अपने क्रान्तिकारी जीवन को पूरी तरह तिलांजलि दे चुके हरदयाल की यह किताब एक तरह की इंसपिरेशनल किताब थी, जिसका आजादी के आन्दोलन से कोई लेना-देना नहीं था। वस्तुस्थिति यह है कि हरदयाल लन्दन में एजवेयर में अपनी ब्रिटिश पत्नी एगडा एरिक्सन के साथ एक सम्पन्न जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी बेहतर थी और उन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति अपनी पहली पत्नी सुन्दर रानी और बेटी शान्ति देवी के नाम कर दी थी। उनकी आर्थिक स्थिति का अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अपने एक पड़ोसी लड़के के लिए भी उन्होंने 200 पाउंड की राशि वसीयत में दी थी, जो उस समय भारत के किराये के लिए काफ़ी थी। उनकी ब्रिटिश पत्नी एगडा एरिक्सन भी काफ़ी अमीर थीं। फ़िलाडेल्फ़िया में जब 4 मार्च, 1939 को उनकी मृत्यु हुई तो वह एक व्याख्यान के सिलसिले में ही वहाँ गए थे, लेकिन इन तथ्यों को किनारे कर 'हरदयाल डे' पर सावरकर एक तरफ़ खुद को उनका नेता बताने पर जोर देते हैं और दूसरी तरफ़ उन्हें पीड़ित और ग़रीब बताकर तालियाँ बजवाने की कोशिश करते हैं।
हद तो यह है कि सावरकर इसके पहले यह भी दावा करने से नहीं चूकते कि अपना घर बेचकर फ्रांस में बम बनाना सीखने गए हेमचन्द्र दास को भी उन्होंने 'अभिनव भारत' की शपथ दिलाई। सावरकर बताते हैं कि हेमचन्द्र बंगाल की ‘मानिकतल्ला' संस्था से थे।" हक़ीक़त यह है कि हेमचन्द्र दास 'अनुशीलन समिति' के सदस्य थे जो बंगाल के क्रान्तिकारी आन्दोलन की सबसे महत्त्वपूर्ण संस्था थी। वह 1907 में फ्रांस गए थे और 1908 में अलीपुर बम कांड में गिरफ्तार होकर उन्हें काले पानी की सजा मिली थी। मानिकतल्ला किसी संस्था का नहीं बल्कि कोलकाता के पास एक जगह का नाम है, जहाँ हेमचन्द्र दास ने अपनी बम फैक्ट्री स्थापित की थी। न तो हेमचन्द्र इंग्लैंड गए, न सावरकर तब तक फ्रांस आए थे तो यह मुलाक़ात और 'अभिनव भारत' की शपथ दिलाने की बात सावरकर द्वारा खुद को सबका नेता बताने के क्रम में एक और प्रवाद है, बस मज़ेदार यह है कि सावरकर इसी क्रम में लिखते हैं कि 'जल्दी ही उनका उल्लेख मुझे करना पड़ेगा, तब उन महान क्रान्तिकारियों का परिचय मैं करा दूँगा, लेकिन इस खंड के अन्त तक हेम बाबू का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता। अंडमान के उनके संस्मरण में भी ऐसा कुछ नहीं है, जिससे उनके हेमचन्द्र दास से पूर्व परिचित होने का कोई संकेत मिले।
'सावरकर : कालापानी और उसके बाद' पुस्तक यहाँ से प्राप्त करें।
