Back to Top
Posted:
November 17, 2023
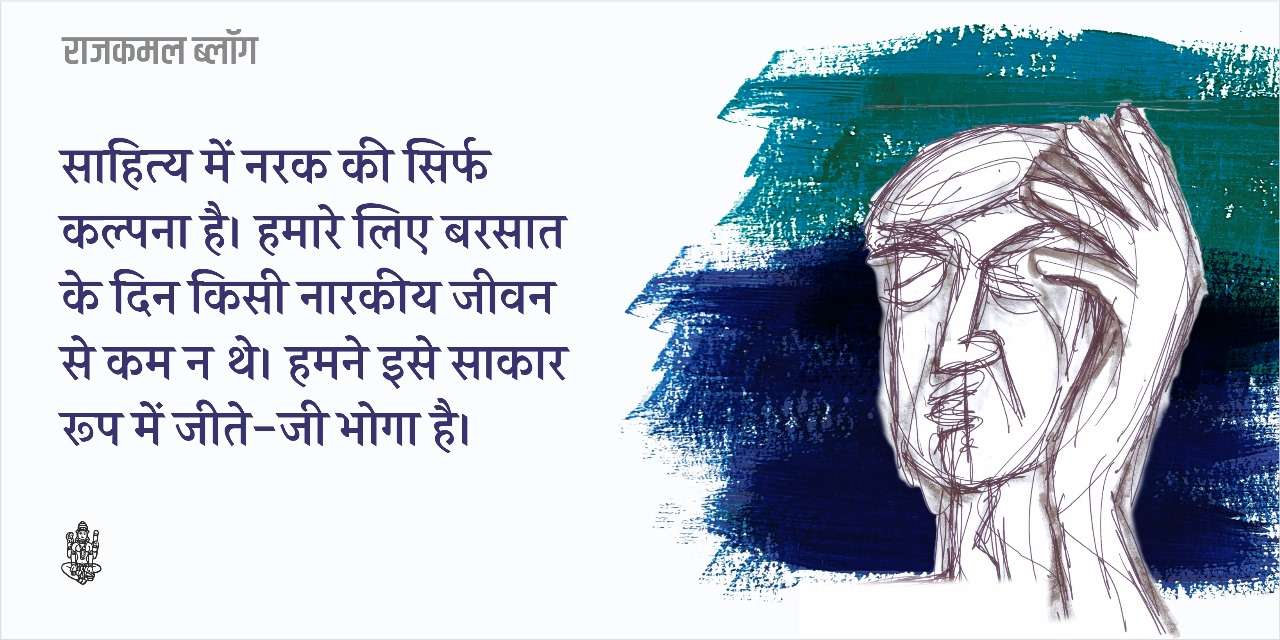
अगले दिन सुबह से लेकर दोपहर तक कोई चूल्हा नहीं जला था। बरसात ने फाकों की नौबत पैदा कर दी थी। जीवन जैसे पंगु हो गया था। लोग गाँव भर में घूम रहे थे, कहीं से कुछ चावल-गेहूँ मिल जाए तो चूल्हा जले। ऐसे दिनों में उधार भी नहीं मिलता। दर-दर भटककर कई लोग खाली हाथ आ गए थे। पिताजी भी खाली हाथ ही आ गए थे। उनके चेहरे पर बेबसी थी। सगवा प्रधान ने अनाज देने की शर्त भी रख दी थी। अपने किसी लड़के को सालाना नौकर रख दो, बदले में जितना अनाज चाहो ले जाओ।
ओमप्रकाश वाल्मीकि की पुण्यतिथि पर राजकमल ब्लॉग में पढ़ें, उनकी आत्मकथा जूठन का एक अंश। इसमें बरसात के दिनों में दलित बस्तियों की दुर्दशा का वर्णन है।
...
1962 के साल में खूब बारिश हुई थी। बस्ती में सभी के घर कच्ची मिट्टी से बने थे। कई दिन की लगातार बारिश ने मिट्टी के घरों पर कहर बरपा दिया था। हमारा घर जगह-जगह से टपकने लगा था। जहाँ टपकता वहीं एक खाली बर्तन रख देते थे। बर्तन में टन-टन की आवाज आने लगती थी। ऐसी रातें जाग-जागकर काटनी पड़ती थीं। हर वक्त एक डर बना रहता था—कब कोई दीवार धसक जाए।
कभी-कभी अचानक ही छत में कोई बड़ा सूराख हो जाता था, जिसे बन्द करना कठिन काम होता था। कच्ची मिट्टी के मकानों की गीली छत और दीवार पर चढ़ना किसी खतरे से कम नहीं होता था।
ऐसी ही एक मूसलाधार बारिश की रात में हमारे घर की छत में एक सूराख हो गया था। छत पर चढ़ने का काम मुझे सौंपा गया था, क्योंकि परिवार में सबसे कम वजन मेरा ही था। तेज बारिश, अँधेरी रात में कुछ सूझ नहीं रहा था। पिताजी के कन्धे पर पाँव रखकर
मैं छत पर चढ़ गया था। पिताजी नीचे खड़े मेरा मार्गदर्शन कर रहे थे, ''सँभल के मुंशी जी, पैरा जमा के...छत पर मत जाणा...दीवाल की तरफ ही रहणा।"
मेरे एक हाथ में बड़ा-सा मिट्टी का ढेला था। दूसरे हाथ से सूराख को ढूँढ़ रहा था अँधेरे में। पिताजी लगातार बोल रहे थे, ''मुंशी जी, मिला गड्ढा..." आखिर सूराख ढूँढ़ने में मैं सफल हो गया था। ढेला रखकर उसे बन्द कर दिया था।
सूराख बन्द करके वापस लौटना मुश्किल हो गया था। तेज बारिश में आँखें खुल नहीं पा रही थीं। पिताजी की आवाज का अन्दाज करके मैं धीरे-धीरे वापस आ रहा था कि अचानक पाँव फिसल गया। क्षण भर को लगा कि मैं हवा में हूँ लेकिन उस अँधेरे में भी पिताजी की अनुभवी आँखों ने मुझे देख लिया था, और मैं उनकी मजबूत पकड़ में आकर सँभल गया था।
मेरी चीख सुनकर माँ भी बाहर आ गई थी। लेकिन मुझे सुरक्षित देखकर आश्वस्त हो गई थी। मैं ठंड से काँप रहा था। मुझे कपड़े से पोंछकर माँ ने चूल्हे के पास बैठा दिया था।
उस रात हमारी बैठक का एक हिस्सा गिर गया था। माँ और पिताजी एक पल के लिए भी नहीं सोए थे। बस्ती में कई मकान गिर गए थे। लोगों के चीखने-चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। पिताजी ने बाहर निकलकर ऊँची आवाज में पूछा था, ''मामू...सब ठीक तो है।" उधर से मामू की आवाज भी उतने ही जोर से आई थी, ''ठीक है...पिछवाड़े की कोठरी गिर गई है।"
सुबह होते ही बस्ती में भगदड़ मच गई थी। हर कोई सुरक्षित जगह की खोज में निकल पड़ा था। बारिश अभी भी जारी थी। बचे-खुचे मकान किसी भी समय गिर सकते थे।
पिताजी सुबह होते ही तगाओं की तरफ चले गए थे। वे जल्दी ही वापस लौट आए थे। आते ही बोले, ''जल्दी करो...मामराज की बैठक खुलवा दी है।" मैंने जल्दी-जल्दी जरूरी चीजें समेट ली थीं। और हम लोग घर का सामान सिर पर रखे बारिश में भीगते हुए मामराज तगा की बैठक में आ गए थे। मामराज की बैठक बरसों से बन्द पड़ी थी। उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता था। दीवारों का प्लास्टर तक उखड़ गया था। फिर भी वह पनाह सुरक्षित थी।
मामराज तगा की बैठक में हमने अभी सामान रखा भी नहीं था कि हमारे पीछे-पीछे तीस-चालीस जन और आ गए थे। बाकी लोग कहीं दूसरी जगह चले गए थे। देखते-ही-देखते बैठक भर गई थी। चारों तरफ सामान-ही-सामान पड़ा था। खाने-पकाने के बर्तनों के साथ जरूरत भर की चीजें थीं। बाकी सब वहीं छोड़-छाड़कर आ गए थे।
इतने लोग एक ही बैठक में समा गए थे। सबसे बड़ी समस्या थी, चूल्हा जलाने की। ईंधन किसी के पास नहीं था। जो था वह बारिश में भीग गया था।
तगाओं के घरों से उपले माँग-माँगकर चूल्हे जलाए गए थे। बैठक में एक साथ आठ-दस चूल्हे बन गए थे। चूल्हे क्या, बस, तीन ईंटों को जोड़कर चूल्हा बन गया था। किसी-किसी को ईंट भी नहीं मिली थी तो ढूँढ़-ढाँढ़कर पत्थर ही जुटा लिये थे। चूल्हों में उठते हुए धुएँ ने बैठक का नक्शा ही बदल दिया था। उस धुएँ में साँस लेना भी मुश्किल था। मर्दों की मंडली बैठक के बरामदे में जमी हुक्के गुड़गुड़ा रही थी। औरतें चूल्हों से जूझ रही थीं। बच्चों की चीख-पुकार ऐसी थी कि कुछ सुनाई ही नहीं पड़ रहा था।
साँझ होते ही बैठक में अँधेरा गहरा गया था। दीया किसी के पास नहीं था। न ही कहीं कोई ढबरी या लालटेन थी। चूल्हों में जलती उपलों की आग अँधेरे से लड़ने का असफल प्रयास कर रही थी। ऐसे वातावरण में आपसी रंजिश भूलकर बस्ती के लोग एक छत के नीचे आ गए थे। जिसके पास जो था उसे बाँटकर खाना चाहते थे।
उस रात माँ ने चने उबाले थे नमक डालकर। यही था रात का हमारा खाना। उस रात उन चनों में जो स्वाद था, जो सन्तुष्टि थी, वैसी सन्तुष्टि मुझे पाँच सितारा होटलों के खाने में भी नहीं मिली।
उस रात किसी चूल्हे पर कोई सब्जी या दाल नहीं पकी थी। रोटी, प्याज और नमक इससे आगे किसी के पास कुछ भी नहीं था।
अगले दिन सुबह से लेकर दोपहर तक कोई चूल्हा नहीं जला था। बरसात ने फाकों की नौबत पैदा कर दी थी। जीवन जैसे पंगु हो गया था। लोग गाँव भर में घूम रहे थे, कहीं से कुछ चावल-गेहूँ मिल जाए तो चूल्हा जले। ऐसे दिनों में उधार भी नहीं मिलता। दर-दर भटककर कई लोग खाली हाथ आ गए थे। पिताजी भी खाली हाथ ही आ गए थे। उनके चेहरे पर बेबसी थी। सगवा प्रधान ने अनाज देने की शर्त भी रख दी थी। अपने किसी लड़के को सालाना नौकर रख दो, बदले में जितना अनाज चाहो ले जाओ।
पिताजी चुपचाप वापस आ गए थे। लेकिन माँ को मामराज तगा के घर से कुछ सेर चावल मिल गए थे जिनसे थोड़ी राहत महसूस की थी हम सभी ने। कई रोज बाद भरपेट खाने का सिला बना था। माँ ने चावल उबालने के लिए चूल्हे पर एक बड़ा-सा बर्तन चढ़ा दिया था। उसमें चावल तो कम थे, लेकिन पानी ऊपर तक भर दिया था। चावल उबलने की महक पूरी बैठक में भर गई थी। छोटे-छोटे बच्चे ललचाई नजरों से चूल्हे की ओर देख रहे थे।
चावल उबल जाने पर पानी अलग कर लिया था। उस पानी के दो हिस्से कर लिये थे माँ ने। एक हिस्से को छौंककर दाल की तरह बना लिया था और दूसरे हिस्से में से सभी बच्चों को एक-एक कटोरी चावल का पानी पीने के लिए दे दिया था। इस उबले चावल के पानी को माँड़ कहते थे। यह माँड़ हम सबके लिए किसी दूध से कम नहीं था। जब भी चावल बनते थे, सभी खुश हो जाते थे, गरम-गरम माँड़ पीकर शरीर में स्फूर्ति आ जाती थी।
बस्ती के पास जुलाहों के घर थे। शादी-विवाह के मौकों पर जब उनकों घरों में दाल-चावल बनते थे, तो हमारी बस्ती के बच्चे बर्तन लेकर माँड़ लेने दौड़ पड़ते थे। फेंक दिया जानेवाला माँड़ हमारे लिए गाय के दूध से ज्यादा मूल्यवान था।
कई बार जुलाहे डाँट-फटकारकर भगाने की कोशिश भी करते थे। लेकिन बच्चे बेशर्म होकर खड़े ही रहते थे। माँड़ पीने का लालच उन्हें डाँट-फटकार से ज्यादा प्रिय था।
माँड़ में नमक मिलाकर पीने से अच्छा लगता था। यदि कभी-कभार गुड़ मिल जाता था तो माँड़ का स्वाद लजीज हो जाता था। माँड पीने की यह आदत किसी शौक या फैशन की देन नहीं थी, अभावों और फाकों से बचने की मजबूरी थी। फेंक देनेवाली चीज हमारी भूख मिटानेवाली थी।
एक बार स्कूल में मास्टर साहब द्रोणाचार्य का पाठ पढ़ा रहे थे। मास्टर साहब ने लगभग रुआँसा होकर बताया था कि द्रोणाचार्य ने भूख से तड़पते अश्वत्थामा को आटा पानी में घोलकर पिलाया था, दूध की जगह। द्रोण की गरीबी का दारुण नक्शा सुनकर पूरी कक्षा हाय-हाय कर उठी थी। यह प्रसंग द्रोण की गरीबी को दर्शाने के लिए महाभारतकार व्यास ने रचा था।
मैंने खड़ा होकर मास्टर साहब से एक सवाल पूछ लेने की धृष्टता की थी। अश्वत्थामा को तो दूध की जगह आटे का घोल पिलाया गया और हमें चावल का माँड़। फिर किसी भी महाकाव्य में हमारा जिक्र क्यों नहीं आया? किसी महाकवि ने हमारे जीवन पर एक भी शब्द क्यों नहीं लिखा?
समूची कक्षा मेरा मुँह देखने लगी थी। जैसे मैंने कोई निरर्थक प्रश्न उठा दिया हो! मास्टर साहब चीख उठे थे, ''घोर कलियुग आ गया है...जो एक अछूत जबान जोरी कर रहा है।"
उस मास्टर ने मुझे मुर्गा बना दिया था। पढ़ाना छोड़कर बार-बार मेरे चूहड़े होने का उल्लेख कर रहा था। उसने शीशम की एक लम्बी-सी छड़ी किसी लड़के को लाने का आदेश दिया था।
''चूहड़े के, तू द्रोणाचार्य से अपनी बराबरी करे है...ले तेरे ऊपर मैं महाकाव्य लिखूँगा..." उसने मेरी पीठ पर सटाक-सटाक छड़ी से महाकाव्य रच दिया था। वह महाकाव्य आज भी मेरी पीठ पर अंकित है। भूख और असहाय जीवन के घृणित क्षणों में सामन्ती सोच का यह महाकाव्य मेरी पीठ पर ही नहीं, मेरे मस्तिष्क के रेशे-रेशे पर अंकित है।
अश्वत्थामा के प्रतिशोध की ज्वाला मैंने अनेक बार अपने भीतर महसूस की है, जो मेरी बेचैनी को बढ़ा देती है।
बरसो-बरस चावल के माँड़ से बनी सब्जी खाकर अपने जीवन के अँधेरे तहखानों से बाहर आने का संघर्ष किया है। माँड़ पी-पीकर हमारे पेट फूल जाते थे। भूख मर जाती थी। यही गाय का दूध था हमारे लिए, यही था स्वादिष्ट भोजन भी। यही था दारुण जीवन जिसकी दग्धता में झुलसकर जिस्म का रंग बदल गया है।
साहित्य में नरक की सिर्फ कल्पना है। हमारे लिए बरसात के दिन किसी नारकीय जीवन से कम न थे। हमने इसे साकार रूप में जीते-जी भोगा है। ग्राम्य जीवन की यह दारुण व्यथा हिन्दी के महाकवियों को छू भी नहीं सकी। कितनी बीभत्स सच्चाई है यह!
ओमप्रकाश वाल्मीकि की पुस्तकें यहाँ से प्राप्त करें।
