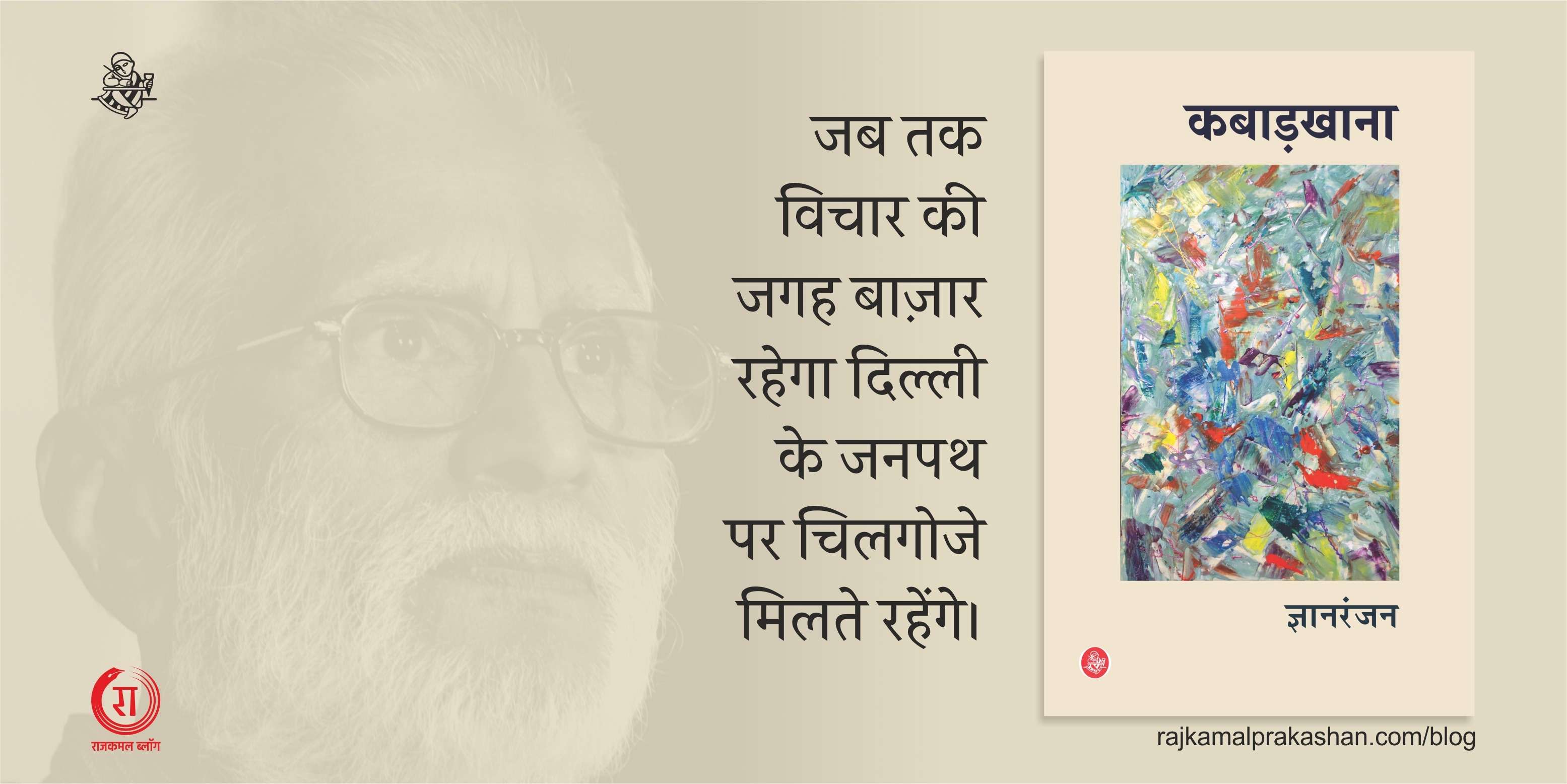
ब्लॉग के इस अंक में पढ़ें, ज्ञानरंजन की किताब 'कबाड़खाना' का अंश नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया।
मुझे यह बात हमेशा से ही बहुत दिलचस्प और चिन्तनीय लगती रही है कि हमारे देश में खासतौर पर हिन्दी के रचनाकारों का दृष्टिकोण नगरों में रहते हुए क्या बन रहा है। आजादी के बाद रोज़गार और परिवर्तन के लाभों को प्राप्त करने के लिए एक आजादी धीरे-धीरे नगरों की तरफ़ आकर्षित होती रही। आज़ादी के बाद ही भारत के नगरों का रूप-परिवर्तन हुआ और अब वे विशालकाय और लुभानेवाले बन गए हैं। दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता, मद्रास के साथ-साथ कुछ और शहर भी उभरे जो आमतौर पर राज्यों की राजधानियाँ हैं। हमारा अधिसंख्य सांस्कृतिक समाज इन्हीं नगरों में केन्द्रित हो गया है। हमारे लेखक, कलाकार छोटी जगहों से बड़ी जगहों की ओर गए हैं क्योंकि उनका यह अन्दाज़ था कि इन नगरों की कला-सृजन की बेहतर सम्भावनाएँ हैं और आधुनिक वातावरण तथा संवेदना के लिए उम्मीदें हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि हुआ कुछ उलटा ही है। चालीस साल में इस आगमन और पलायन के बाद भी हमारे सर्जक की वह मध्यवर्गीय पोटली कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है और वह आज तक अपनी स्मृतियों से बाहर नहीं आ सका है। शहर से न तो वह पूरी तरह टकरा रहा है और न शहको सही मायनों में स्वीकार कर पा रहा है। जिस तरह मिर्जा ग़ालिब रहे थे, और टकराए थे, उस तरह भी नहीं।
मुझे नगरों से गहरा लगाव या कि प्रेम रहा है जबकि मैंने नगरों में रहने का चुनाव कभी नहीं किया। पर मैं एक छोटे नगर में इसलिए नहीं हूँ कि बड़े नगरों को आमतौर पर कोसा जाए, उनकी आलोचना, निन्दा इस वजह से की जाए कि वे पत्थर हृदय हैं। पत्थर दिल नगर-यह एक ऐसा जुमला है जो अन्तिम और उखड़ी हुई रूमानियत की साँस ले रहा है।
नगर बनते हैं और नगर समाप्त हो जाते हैं। बर्लिन की आत्मा गुम हो गई है, पेरिस का आवेग ढह गया, लन्दन का सांस्कृतिक दर्प खो गया, मारियो की बम्बई धूमिल पड़ रही है और दिल्ली तो सौ-सौ बार बदली। अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने अपने बदतर दिन पेरिस में बिताए और कहा कि जो बातें हम किसी दूसरे शहर में दस साल में भी नहीं सीख पाते वह पेरिस हर मिनट हमें सिखाता है। लेनिन ने अपने अन्तिम दिनों में मास्को शहर को देखने की इच्छा प्रकट की थी। विख्यात कवि पाब्लो नेरूदा अपनी जन्मभूषि के जंगलों और नदियों और अगम्य इलाक़ों को छोड़ किन-किन नगरों में नहीं रहे । प्रेमचन्द जैसे ग्रामीण व्यक्ति भी बम्बई का लोभ नहीं छोड़ सके। उग्र गए बम्बई और हरिकृष्ण प्रेमी गए और अश्क गए और अमृतलाल नागर गए, क़ैफ़ी गए, बेदी गए और लगातार यह सिलसिला बना रहा। लेकिन कोई भी लेखक नगर-संस्कृति को स्वीकार नहीं कर सका। बीजों से निकलनेवाले पौधे रोपे नहीं जा सके। इसे मैं समूचे परिदृश्य के हिसाब से गहरा आघात मानता हूँ।
'मुझे यह गाना अच्छा लगता है और यह पंक्ति कि इस शहर में हर शख्स परेशान-सा क्यूँ है, लेकिन इसका विचार मुझे नापसन्द है। इसलिए कि नगर-संवेदना के लिए यहाँ चुनौतियाँ हैं, यहाँ मानव-जाति को पनाह है और यहाँ आप अपने सृजन में असफल होकर भी एक अच्छे समुन्नत नागरिक बन सकते हैं। हिन्दी का लेखक क्यों नहीं बन सका ? इसका सबब खोजना होगा। इसका भी कि हिन्दी का लेखक नगर-सभ्यता से इतना हताश क्यों है ?
लोग मालगुडी डेज और विन्सबर्ग ओहियो क्यों पसन्द करते हैं ? इसलिए कि इन क़स्बाई कहानियों से वे आगे नहीं जा सके। इसीलिए उन्हें कमलेश्वर की दिल्ली में एक मौत पसन्द आती है और श्रीकान्त वर्मा का कलिंग के नाम पर लगातार रोना। हमारे साहित्य-रसिकों को यह काव्य हरक़त पसन्द आती है। हमारे साहित्यकार शहर में रहक़र शहर से दूर हैं। आप किसी भी दिल्ली-बसे लेखक से बात करें, मिलते ही वह सबसे पहले अपने ही नगर पर एक आघात-भरी टिप्पणी करेगा। वह हमेशा चिढ़ा हुआ रहता है। वास्तव में वह प्रवासी है, उसने नगर को कभी स्वीकार नहीं किया और इसी को वह अपनी सार्थक्ष आधुनिकता मानता है। उसे नगर की आलोचना करने की अपार फूर्सत है। वह बन्द अँधेरे कमरे लिखता है, वह दिल्ली मेरा परदेस लिखता है। अपने साहित्यिक जीवन की पूरी कमाई शैलेश मटियानी ने बम्बई में रहकर की पर अन्ततः भाग खड़े हुए। दो तरह के हिन्दी लेखक हैं, एक तो वे जो नगरों में गए और वहाँ से लौट आए जैसे प्रेमचन्द या शैलेश मटियानी। दूसरी कोटि के वे लेखक हैं जो नगरों में रह रहे हैं और जीवन तथा साहित्य में कराह रहे हैं। जब सुप्रसिद्ध ग्रीक कवि कवेफी ने अपनी “बारबेरियंस आर कमिंग” कविता में लिखा कि जल्लाद लोग आ रहे हैं तो वे अपने नगर के प्रति गहरा प्यार प्रदर्शित कर रहे थे। और जब अशोक वाजपेयी ने अपने कविता-संग्रह का नाम दिया शहर अब भी सम्भावना है, तो अशोक वाजपेयी ने संयत मुहावरे का प्रयोग किया है। धर्मवीर भारती ने जिस इलाहाबाद का विवरण गुनाहों के देवता में दिया है, वह गहरा रूमानी है; नागरजी. ने लखनऊ के प्रति जो लगाव दिखाया है, वह सामन्ती गुण की पहचान है और केदारनाथ अग्रवाल ने बाँदा और केन नदी के इलाक़े को नहीं छोड़ा तो यह उनकी अपनी धरती का सघन रिश्ता है। परसाई ने जबलपुर छोड़ जब सागर तक को बर्दाश्त नहीं किया तो यह उनका आदिम भय था। वे होशंगाबाद छोड़कर आ गए लेकिन दूसरी उड़ान के लिए तैयार नहीं हुए। दिनकर दिल्ली के स्थायी बाशिंदा कभी-कभी रहे लेकिन उन्होंने अपनी लम्बी कविता दिल्ली में उसके बदलते रहते स्वरूप को सम्मानजनक रूप में स्वीकार नहीं किया। यह एक अत्यन्त दिलचस्प सूचना है कि रूमानी दृष्टिकोण के बावजूद उर्दू के कवि-कथाकारों ने बड़े नगरों ज़्यादा हौसले से स्वीकार किया है।
जब हम रोजगार के लिए नगरों में जा रहे हैं तो भीड़, दुर्घटना, प्रदूषण होगा और पसीने से तरबतर स्त्रियाँ बस के लिए भागती हुई ज़रूर मिलेंगी। कृपया शहर के भीतर जाइए। जब तक विचार की जगह बाजार रहेगा दिल्ली के जनपथ पर चिलगोजे मिलते रहेंगे। नगर के वास्तविक हादसे की तरफ़ हमारा ध्यान नहीं है। वास्तव में हम एक नर्क से दूसरे नर्क में यात्रा करते हैं लेकिन यह सच्चाई को न जानकर एक फ़र्क़ अपनी सोच में पैदा करते हैं। सलाम बॉम्बे और महानगर के बावजूद नगर व्यर्थ नहीं है। मुझे कुछ दिन पहले सत्यजित राय के उस कथन पर बहुत कोफ्त हुई थी कि कलकत्ता मर गया है। क्षमा माँगते हुए लिखना चाहूँगा कि यह सत्यजित राय का बुढ़ापा और उनकी मृत्यु है। इस नगर ने ही उन्हें उच्चतर कला संस्कार दिए। मुझे तब भी अच्छा नहीं लगा जब खुशवन्त सिंह ने अपनी किताब दिल्ली में दिल्ली के बारे में बड़े चालू तरह से पत्रकारितापूर्ण टिप्पणी की या निष्कर्ष निकाले। आप शराब पीकर शहरों पर टिप्पणी करने के हक़दार नहीं हैं। लगता है कि लोग शहरों पर पिल पड़े हैं। रात की बाँहों के रुमान से लेकर आजकल महानगरों पर लिखी जानेवाली टिप्पणियों में बौद्धिक दिवालियापन ही नजर. आता है और इसके लिखनेवाले हिन्दी के आधुनिक युवा कवि-कहानीकार हैं। हमें नगर के बारे में अब गहरी तैयारी और सघन सूझ-बूझ से लिखना होगा जिसमें समूचे मुल्क के भीतरी परिवर्तन शामिल होंगे। हम प्रचलित घड़ियों में समय देखना बन्द कर दें अन्यथा गलत समय का पता मिलेगा। एक बार नरेश मेहता ने छदम आधुनिकता से ओतप्रोत शिवप्रसाद सिंह के एक हिन्दी उपन्यास पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि “इसे पढ़कर लगता है कि एफल टावर पर ददरी का मेला लगा हुआ है” जब आप मीनमेख कर रहे होते हैं, कोसते रहते हैं, उस समय मत भूलिए कि शहर को असंख्य लोग प्यार करते होते हैं। असंख्य लोग उसी शहर में पनाह लेते होते हैं। ये ही लोग होते हैं जो नगरों को बचाते हैं। अल्पविरामी, प्रवासी और हमलावर मानसिकता के लोग शहर पर काबिज हैं, हिन्दी पर और गलत टिप्पणी इतिहास में दर्ज कर रहे हैं। अज्ञेय ने शायद तीन दशक पूर्व ठीक लिखा था:
साँप
तुम सभ्य तो हुए नहीं
नगर में बसना
भी तुम्हें नहीं आया
ज्ञानरंजन की किताबें यहाँ उपलब्ध हैं।
