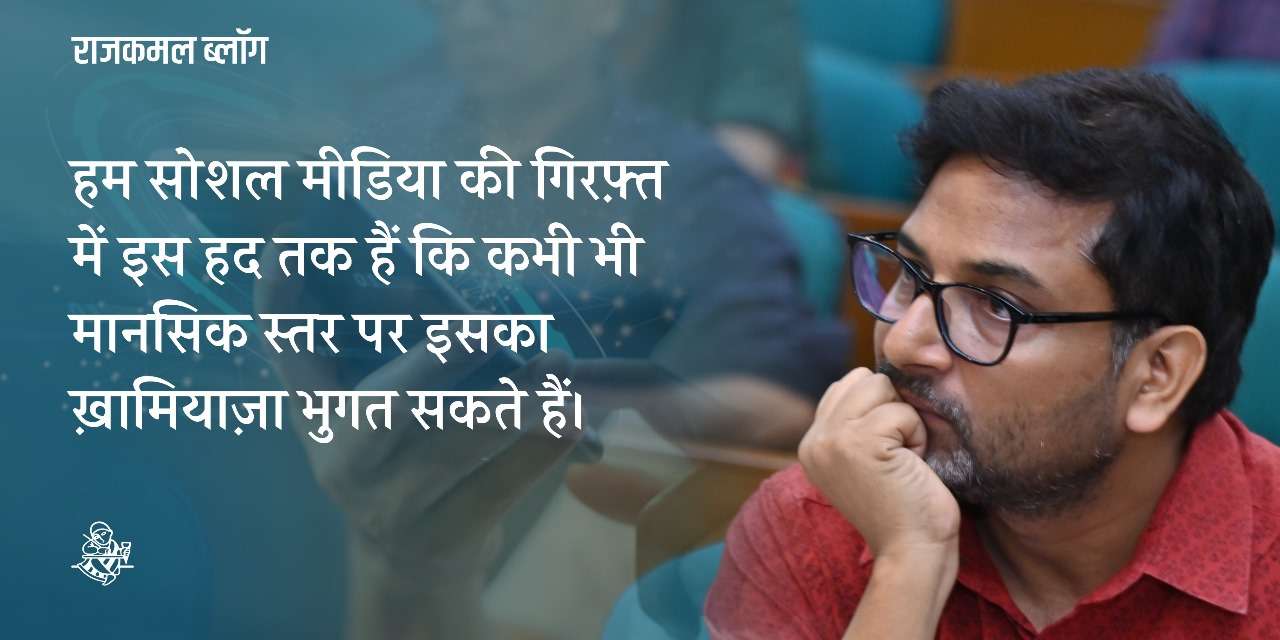
“मैं अपने आसपास के लोगों को देखता हूँ कि वे बातचीत की शुरुआत करने के पाँच से सात मिनट के बाद उसे उन प्रसंगों से जोड़ने लग जाते हैं कि मोबाइल फ़ोन निकालकर कोई तस्वीर, लिंक या पोस्ट दिखाने की ज़रूरत पड़ जाए। कई बार वे फ़ोन पर इनबॉक्स कर देते हैं। उसके बाद वे कुछ और देखने लग जाते हैं या फिर दूसरा प्रसंग ऐसा छेड़ते हैं कि फिर मोबाइल की ज़रूरत पड़ जाए।”
मोबाइल फोन पर दिनभर उगलियाँ चलाते रहना लगभग हम सबकी एक आदत हो चली है। इसके फायदे-नुकसान पर भी अक्सर बहसें होती है। कई लोग सोशल मीडिया के नुकसानों के बारे में बताते हुए उन्हीं प्लेटफॉर्म पर विडियो/लेख आदि शेयर करते रहते हैं। वहीं कुछ लोग सोशल मीडिया के इस्तेमाल को कम करने या बिलकुल नहीं करने की शपथ लेकर कुछ ही दिनों में वापस इसे इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं। इन सबको देखते हुए हमारे मन में इसको लेकर कई तरह के सवाल उठते हैंं। ऐसे ही सवालों से जूझते और उनका जवाब तलाशने की कोशिश करते हुए प्रतिष्ठित मीडिया विश्लेषक और दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर विनीत कुमार ने ‘आलोचना’ पत्रिका के अंक-72 में एक विस्तृत और शोधपरक लेख लिखा है, जिसका शीर्षक है : ‘डिजिटल डिटॉक्स’ : माध्यमों की ज़रूरत और लत के बीच की बहस। राजकमल ब्लॉग में पढ़ें, इस लेख का एक अंश।

…
दुनिया में एक के बाद एक जितने भी नए माध्यम आए हैं उनके आने के साथ ही दो सिरे से विमर्श चलते रहे हैं—एक तो यह कि उनके होने से मनुष्य का जीवन कितना सहज, बेहतर और आपस में संबद्ध हुआ है और दूसरा कि उसकी प्रकृति के कारण किस तरह के प्रभाव पैदा होते हैं और उनसे क्या नुक़सान हैं? माध्यमों की प्रकृति के सिरे से ख़ास तौर पर टेलीविज़न के आने के बाद से विमर्श का सिलसिला कहीं ज़्यादा व्यवस्थित ढंग से शुरू हुआ। रेमंड विलियम्स ने तकनीक को मानव-सापेक्ष बताते हुए भले ही उसके प्रयोग किए जाने के अनुसार नफ़ा-नुक़सान की बातें विस्तार से अपनी किताब टेलीविज़न : टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल फ़ॉर्म (1974) में की, लेकिन वहीं मार्शल मैक्लूहान ने माध्यमों की प्रकृति के अनुरूप मनुष्य पर पड़नेवाले इसके प्रभाव का अध्ययन किया। वो अपनी किताब अंडरस्टैंडिंग मीडिया : दि एक्सटेंशन ऑफ़ मैन (1964)20 के दूसरे अध्याय ‘मीडिया हॉट एंड कोल्ड’ में माध्यमों का विभाजन करते हुए टेलीविज़न को जब ठंडा माध्यम बताते हैं तो उसके पीछे उनका तर्क है कि यह हमारी कल्पनाशीलता, रचनात्मकता और सक्रियता को शिथिल करने का काम करता है। इसका चरित्र ऐसा है कि हम उससे परे कुछ और सोच नहीं पाते। मैक्लूहान इसके लिए ‘हाय डेफ़िनिशन’ शब्द का प्रयोग करते हैं जिसका आशय है कि ऐसा माध्यम जिसमें कि संप्रेषण के सारे कारक मौजूद हों। सुनने में तो हमें यह बड़ा अच्छा लगता है कि सही तो है कि एक ही माध्यम में सूचना, ज्ञान, भाव एवं संवेदना के सारे कारक मौजूद हैं लेकिन मैक्लूहान इसे मनुष्य की प्रकृति और उसके मस्तिष्क के लिए ठीक नहीं मानते। उनके अनुसार, जिस माध्यम में जितने कम कारक होंगे, मनुष्य उसके ज़रिये ज्ञान को लेकर उतना अधिक समृद्ध, रचनाशील और जानकारी हासिल करने के प्रति सक्रिय हो सकेगा।
इंटरनेट और सोशल मीडिया के तक़रीबन पचास साल पहले मार्शल मैक्लूहान की इस गरम माध्यम और ठंडे माध्यम की अवधारणा की जमकर आलोचना हुई। रेमंड विलियम्स इसे मानव-सापेक्ष बताकर मैक्लूहान के तर्कों का खंडन ही करते हैं जिसके संकेत उनकी किताब में लगातार मिलते हैं। इसके साथ ही जॉन फ़िस्के और जॉन हर्टली ने रीडिंग टेलीविज़न (1978) में तो इस तर्क को ही उल्टा खड़ा कर दिया कि दरअसल टेलीविज़न की आलोचना किए जाने के पीछे यथार्थ को लेकर जो तर्क प्रस्तावित किए जाते हैं, वही अपने आपमें भ्रामक हैं। सच तो यही है कि यथार्थ स्वयं में निर्मित की जानेवाली चीज़ है और यह व्यक्ति और संस्थान के हाथ में है कि वह अपनी सुविधा और ज़रूरत के अनुसार किस तरह के यथार्थ की निर्मिति करता है? इसी क्रम में वे इसे स्वतंत्र माध्यम न मानकर पूर्ववर्ती माध्यमों के समुच्चय के रूप में देखने की बात करते हैं।
लेकिन मार्शल मैक्लूहान की माध्यम संबंधी यह अवधारणा इतनी लोकप्रिय और मीडिया एवं सांस्कृतिक अध्ययन के संदर्भ में इस हद तक स्थापित है कि हर नए माध्यम के आने के बाद एक बार पीछे मुड़कर देखना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। मार्शल मैक्लूहान के हिसाब से सोचिए तो टेलीविज़न ठंडा माध्यम है क्योंकि इसमें एक ही साथ ध्वनि, दृश्य, रंग और गति सब शामिल होते हैं और ऐसा होने से मनुष्य की रचनात्मकता एवं दिमाग़ी स्तर का सुकून भंग होता है तो फिर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का सोशल मीडिया किस हद तक जाता है? ज़ाहिर है कि यह सवाल महज़ उसकी सामग्री के स्तर पर नहीं, उसकी प्रकृति को लेकर भी है। इधर जॉन फ़िस्के के अनुसार टेलीविज़न यदि पूर्ववर्ती माध्यमों का समुच्चय है तो इस क्रम में सोशल मीडिया को देखा जाए तो यह समुच्चयों का समुच्चय हुआ। हम-आप समुच्चयों के समुच्चय इस माध्यम पर छह-आठ-दस...घंटे जो बिता रहे होते हैं, उस दौरान लगातार हम सरोकारी, मानवीय पक्ष एवं संवेदना से जुड़ी सामग्री साझा करते हुए अपने को ‘गिल्ट फ़्री ज़ोन’ में ले जाने की कोशिश करते हैं, अपने आसपास की बौद्धिक ज़मात को सक्रिय देखकर आश्वस्त होते हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन इस सिरे से शायद नहीं सोचते कि सामूहिक स्तर पर प्रभाव पैदा करने के क्रम में व्यक्तिगत स्तर पर हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं और क्या हम कभी महसूस भी करते हैं कि हमें इस माध्यम से थोड़े समय के लिए दूर हो जाना चाहिए? यदि हम ऐसा सोचना शुरू करें और अपने को इससे काटने की कोशिश करें और इस कोशिश में अड़चनें आने लग जाएँ तो यह इस बात का संकेत है कि हम सोशल मीडिया की गिरफ़्त में इस हद तक हैं कि कभी भी मानसिक स्तर पर इसका ख़मियाज़ा भुगत सकते हैं। यह स्वभाव में चिड़चिड़ेपन से लेकर किसी काम में मन न लगने, ध्यान भटक जाने, भूलने लग जाने और आभासी स्तर पर समस्याओं का हल निकालने के तौर पर हो सकता है। ऐसे लोगों से आप बात करते हुए भी जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते हैं और पूरा समय इस आशंका में निकल सकता है कि पता नहीं कब ये वापस स्क्रीन की दुनिया में खो जाएँगे।
मैं अपने आसपास के लोगों को देखता हूँ कि वे बातचीत की शुरुआत करने के पाँच से सात मिनट के बाद उसे उन प्रसंगों से जोड़ने लग जाते हैं कि मोबाइल फ़ोन निकालकर कोई तस्वीर, लिंक या पोस्ट दिखाने की ज़रूरत पड़ जाए। कई बार वे फ़ोन पर इनबॉक्स कर देते हैं। उसके बाद वे कुछ और देखने लग जाते हैं या फिर दूसरा प्रसंग ऐसा छेड़ते हैं कि फिर मोबाइल की ज़रूरत पड़ जाए। एक घंटे की बातचीत में ऐसा वे दस से बारह बार करते हैं और एक स्थिति ऐसी भी आती है कि वे मोबाइल में रम जाते हैं और बातचीत का सिरा हवा में लटकता रह जाता है। इस बीच कई बार सॉरी-सॉरी और फिर वापस मोबाइल स्क्रीन पर झुकी आँखें! ऐसे लोगों के बीच से दस मिनट के लिए मोबाइल ग़ायब कर दिए जाएँ तो वे बेचैन हो उठते हैं। संभवतः यह सब देखकर आपको ग़ुस्सा आए, उनके इस व्यवहार से आप अपमानित महसूस करें और दोबारा उनके पास न जाना चाहें। लेकिन इन लक्षणों पर ग़ौर करें तो दरअसल वे ‘नोमोफ़ोबिया’ के शिकार व्यक्ति हैं जिन्हें मोबाइल फ़ोन हाथ में, पास में न होने पर घबराहट होने लगती है, लगता है, कोई चीज़ पीछे छूट जा रही है। यही स्थिति हाथ में मोबाइल होने पर बार-बार स्क्रीन देखने या स्क्रोल करने को लेकर होती है और ऐसे व्यक्ति ये सब करते हुए घंटों समय बिता सकते हैं। आपके साथ होते हुए भी व्यवहार से जतला देते हैं कि अभी के लिए इतना ही, फिर मिलना होता रहेगा। लेकिन आप जैसे ही उनसे छूटते हैं, इनबॉक्स में दोबारा से बातचीत शुरू हो जाती है। सामने बैठे होने पर जिनकी समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या बात करें, इनबॉक्स में उनकी ओर से एक के बाद एक बेहद ही सहज अंदाज़ में बातें सामने आने लग जाती हैं। ये सारे लक्षण बताते हैं कि वे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और सोशल मीडिया की जकड़ में हैं और इससे निकलने के लिए डिजिटल डिटॉक्स किसी भी बीमारी के इलाज की तरह ही ज़रूरी है।
‘आलोचना’ पत्रिका की सदस्यता यहाँ से प्राप्त करें।
