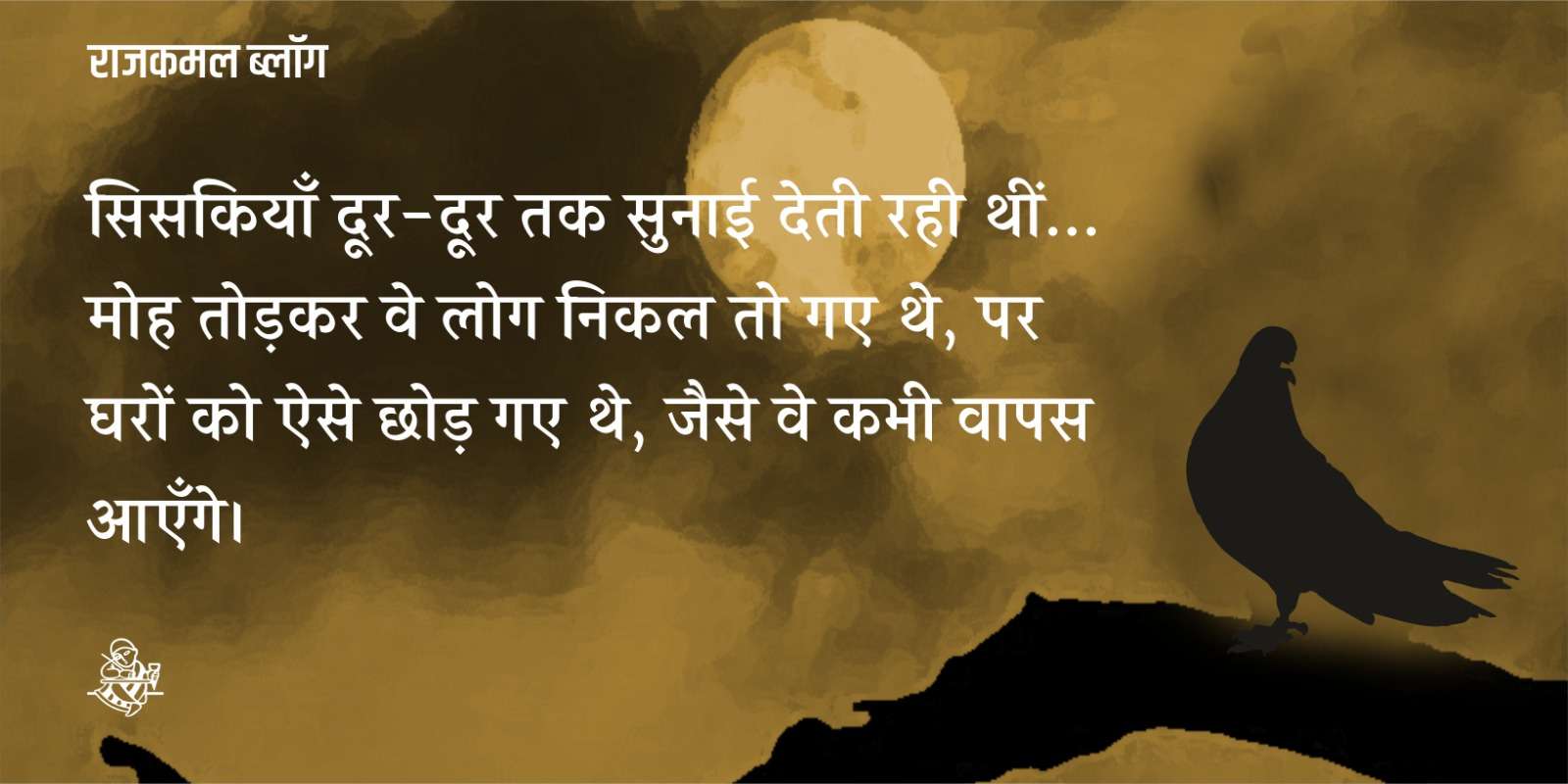
विभाजन हुआ तो पंजाब में खून की नदियाँ बहीं... बंगाल में मार-काट हुई। सूबे के बड़े शहरों में कत्ल हुए और बस्तियाँ जलाकर राख कर डाली गईं...।
पर इस शहर में एक बूँद खून नहीं गिरा। किसी मुहल्ले पर धावा नहीं हुआ। किसी ने किसी को नहीं मारा। किसी ने किसी को गाली तक नहीं दी। मस्जिदों में लड़ाई की तैयारियाँ नहीं हुईं, मन्दिरों में ईंट-पत्थर इकट्ठे नहीं हुए, जो बदमाश रोज पिटते थे, उन्हें भी किसी ने नहीं पीटा।
लेकिन भीतर ही भीतर एक भूचाल आया हुआ था जिससे बस्ती की चूलें हिल रही थीं। दिली इमारतें ढह रही थीं। एक उबलता हुआ नफरत का दरिया नीचे ही बह रहा था...शक और डर सबके दिलों में समाए हुए थे।
कमलेश्वर की जयंती पर राजकमल ब्लॉग में पढ़ें, उनके उपन्यास ‘लौटे हुए मुसाफिर’ का एक अंश। वर्ष 1961 में प्रकाशित इस उपन्यास में स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ गम्भीर रूप धारण करती साम्प्रदायिकता की समस्या और भारत विभाजन के नाम पर बेघर-बार हुए मुस्लिम समाज के मोहभंग और उनकी वापसी की विवशता को दर्शाया गया है।
...
सब कुछ अपनी जगह पर था― पर कुछ था जो नहीं था। गलियों के छोटे-छोटे घरों में बैठे सुनार जेवर गढ़ रहे थे। तालाबों में कमल फूले हुए थे। जलमंजरी के पत्ते नागों की तरह फन उठाए हुए खड़े थे। जंगल में कमरख और आँवले फले थे।
झाड़ियों में मधुमक्खियों के छत्ते अब नहीं थे, पर मन्दिरों के आँगनों में कनेर अब भी फूले हुए थे और मस्जिदों के सहन में मेहँदी महक रही थी।
पर वातावरण में आशंकाएँ रेंग रही थीं...
एक भयानक खौफ लोगों के दिलो-दिमाग पर हावी था...।
विभाजन हुआ तो पंजाब में खून की नदियाँ बहीं... बंगाल में मार-काट हुई। सूबे के बड़े शहरों में कत्ल हुए और बस्तियाँ जलाकर राख कर डाली गईं...।
पर इस शहर में एक बूँद खून नहीं गिरा। किसी मुहल्ले पर धावा नहीं हुआ। किसी ने किसी को नहीं मारा। किसी ने किसी को गाली तक नहीं दी। मस्जिदों में लड़ाई की तैयारियाँ नहीं हुईं, मन्दिरों में ईंट-पत्थर इकट्ठे नहीं हुए, जो बदमाश रोज पिटते थे, उन्हें भी किसी ने नहीं पीटा।
लेकिन भीतर ही भीतर एक भूचाल आया हुआ था जिससे बस्ती की चूलें हिल रही थीं। दिली इमारतें ढह रही थीं। एक उबलता हुआ नफरत का दरिया नीचे ही बह रहा था...शक और डर सबके दिलों में समाए हुए थे।
दूसरे शहरों, कस्बों और सूबों से तरह-तरह की खौफनाक खबरें आ रही थीं। हर सुबह एक नई खबर होती-हर शाम एक और नया डर होता।
ठहरी-ठहरी शामें थीं और वक्त जैसे रुका हुआ था। कोई किसी से कुछ नहीं कहता था। एक अजीब-सा तनाव था दोनों तरफ।
सुबह होती, फिर उदास-सी शाम उतर आती। मुसलमानों का कारोबार ठप्प हो गया था। जिन्दगी जैसे रुक गई थी।
तभी और खबरें आई थीं―
अलीगढ़ से मुसलमानों का एक जत्था पुलिस की देख-रेख में रेल से लाहौर जा रहा है―पाकिस्तान।
अहमदाबाद के मौलवी साहब और उनका पूरा घराना कल ही कराँची के लिए रवाना हो गया―पाकिस्तान।
कोसमा के जमींदार अब्दुल हक साहब का घराना कल लाहौर जा रहा है―पाकिस्तान।
पाकिस्तान जानेवाले हर मुसलमान के लिए जिन्ना साहब की सरकार ने पूरा इन्तजाम किया है। पाकिस्तान जानेवालों के लिए जिन्ना साहब ने अपनी फौज भेजी है जो उन्हें हिन्दुओं के इलाकों से बाहिफाजत निकाल ले जाएगी...।
तभी यासीन ने एक तूफानी दौरा किया था― "गांधी की बातों पर यकीन मत कीजिए। वह चाहता है कि मुसलमानों को यहीं रोककर बाद में मरवा डाला जाए। यह फरेब है। पाकिस्तान बना ही इसीलिए है कि हर मुसलमान वहाँ आराम और चैन से रहे। सारे इन्तजामात पूरे हो गए हैं। हवाई जहाज दिल्ली के अड्डे पर इन्तजार कर रहे हैं... पाकिस्तान की सरहद पर ही जमीनें और जायदादें बँट रही हैं, काम-धन्धे शुरू करने के लिए जिन्ना साहब की सरकार नकद रुपए दे रही है। अंगूर आठ आने सेर बिक रहा है..."
आस-पास कस्बों से पुराने मुसलमान जमींदारों के घरानों की खबरें भी आती रहीं-बेदगाँव के सैयद साहब भी आज चले गए। अटाला के हकीम जी भी चले गए।
शहर कोतवाल ने हिन्दुस्तान की नौकरी छोड़कर पाकिस्तान जाने का तय किया है। डिप्टी कलेक्टर खान साहेब भी इस्तीफा देकर अपने शहर गाजीपुर गए हैं, वहाँ के हवाई जहाज से वे कराँची जा रहे हैं― कराँची यानी पाकिस्तान।
और उसे शाम हाफिज जी जब अपनी दुकान का सामान लदवाकर घर की तरफ चले, तो शर्बत वाले सन्ता ने उन्हें गौर से देखा। हाफिज जी ने मुस्कराकर दूर से ही सलाम किया और बोले, "खाली नहीं कर रहा हूँ।"
पर सुबह एक मोटर में सारा सामान भरकर हाफिज जी अपने बाल-बच्चों समेत निकल गए। घर एक दर्जी को सौंप गए। किसी को पता नहीं चला कि हाफिज जी कब और क्यों चले गए।
सभी गरीब मुसलमानों की निगाहें अमीर लोगों की तरफ लगी थीं―जो वे करेंगे वही ठीक होगा।
एकाएक कुछ चेहरे शहर से गायब हो गए... वे चेहरे जो चुंगी में लोगों की रहनुमाई करते थे, स्कूल की कमेटियों में बहस करते थे। तहसील-कचहरियों में पैरवी करते थे...।
माजिद साहब की कोठी के बाहर के पौधे सूखने लगे तो पता चला कि चार दिन हुए वे भी पाकिस्तान चले गए। गुलाम नबी मोटरवालों का पता ही नहीं चला... उनकी मोटरें वैसे ही धूल उड़ाती हुई जसराना लाइन पर दौड़ती रहीं, पर बाद में मालूम हुआ कि वे अपनी मोटरें और हवेली एटा के मारवाड़ी के हाथ बेचकर चुपचाप चले गए।
कुछ चेहरे थे जो शाम तक हँसते-मुस्कराते दिखाई पड़ते थे पर सुबह बगैर सलाम-बन्दगी के खो जाते थे।
सहसा कुछ घरों में रात में रोशनी नहीं हुई तो लगा कि खाली हो गए।
शहर की कुछ दुकानों के पटरों पर तीन-तीन, चार-चार दिनों का कूड़ा जमा दिखाई दिया तो मालूम हुआ कि वे सौदागर भी चले गए।
जितने भी पैसे वाले थे, वे जल्दी-से-जल्दी अपना इन्तजाम करके चले गए। गरीबों का कोई रहनुमा नहीं था। चिकवों की बस्ती में लोगों का यही खयाल था कि यासीन भी अलीगढ़ गया है, और वहाँ से लाहौर चला गया होगा, पर दस रोज बाद ही यासीन लौट आया और उसने बताया― "भई, काम और भी थे लाखों की तादाद में लोगों को चलना है। उनका इन्तजाम भी तो होना था।"
और एक रात चिकवों की बस्ती के बाशिन्दों की यात्रा का प्रबन्ध हुआ।
सब कुछ खामोशी और चुपके-चुपके हुआ।
शाम को तय हो गया था कि परसों सवेरे, सूरज उगने से पहले यहाँ से काफिला निकल पड़ेगा-और यासीन उन्हें दिल्ली स्टेशन पर मिलेगा, वहाँ से रेलों या हवाई जहाजों द्वारा उन्हें पाकिस्तान पहुँचाया जाएगा...
निश्चित दिन तीन बजे रात को ही दस घरानों का एक काफिला बस्ती से रवाना हुआ-अपना सामान, चीज-बस्त और बाल-बच्चों को लेकर...।
"खुदा हाफिज!"
आँसू, दुख और घरों को छोड़ने की तकलीफ।
सिसकियाँ दूर-दूर तक सुनाई देती रही थीं... मोह तोड़कर वे लोग निकल तो गए थे, पर घरों को ऐसे छोड़ गए थे, जैसे वे कभी वापस आएँगे।
रात अँधेरी थी और स्टेशनवाला रास्ता सुनसान था। सबों ने पैसे जुटाकर तीन बैलगाड़ियाँ किराए पर ली थीं, जो उन्हें जंक्शन तक पहुँचाकर वापस आएँगी। अपने स्टेशन से गाड़ी में बैठना ठीक नहीं― यह यासीन ने ही बताया था।
सुबह नसीबन मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठी-बैठी उन वीरान घरों को देखती रही, जिनके बाशिन्दे चले गए थे... आसमान उदास था और पजावों के पीछे आज हद से ज्यादा सन्नाटा छाया हुआ था।
उस दिन लोगों के पास बात करने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। सत्तार निढाल-सा घर में पड़ा था और इफ्तिकार अपनी कोठरी में बैठा घोड़े के घुँघरू बजा-बजाकर कुछ गा रहा था। बहुत देर तक नसीबन उन उजड़े हुए घरों को देखती रही फिर उसने अपनी आँखें सुखाई और सीढ़ियों से उतरकर घर चली आई। बस्ती में ऐसी भयानकता छाई हुई थी जैसे दस-बीस मौतें एक साथ हो गई हों। दोपहरी सायँ-साय करती रही।
दोपहर बाद सत्तार उठा था, घड़े से पानी पीकर जरा ठीक हुआ तो नसीबन से बोला था― "कल मैं भी जा रहा हूँ।"
"अच्छा।"
फिर बहुत देर चुप्पी छाई रही।
कुछ आहट हुई तो सत्तार ने देखा― इफ्तिकार खड़ा था। धीरे से भीतर जाकर वह बोला― "सलमा ने तुझे बुलाया है...।"
"कहाँ?"
"मस्जिद के पास, यहाँ वह नहीं आना चाहती।"
सत्तार उठकर चला गया। इफ्तिकार बैठा रहा पर नसीबन से कोई बात ही नहीं हुई। आखिर इफ्तिकार ने ही खामोशी तोड़ी थी―
"तुम जा रही हो...।"
"कहाँ जाऊँगी?"
"जहाँ और सब जा रहे हैं।"
नसीबन हँस दी थी। उसकी हँसी में कोई अर्थ नहीं था।
कमलेश्वर की पुस्तकें यहाँ से प्राप्त करें।
