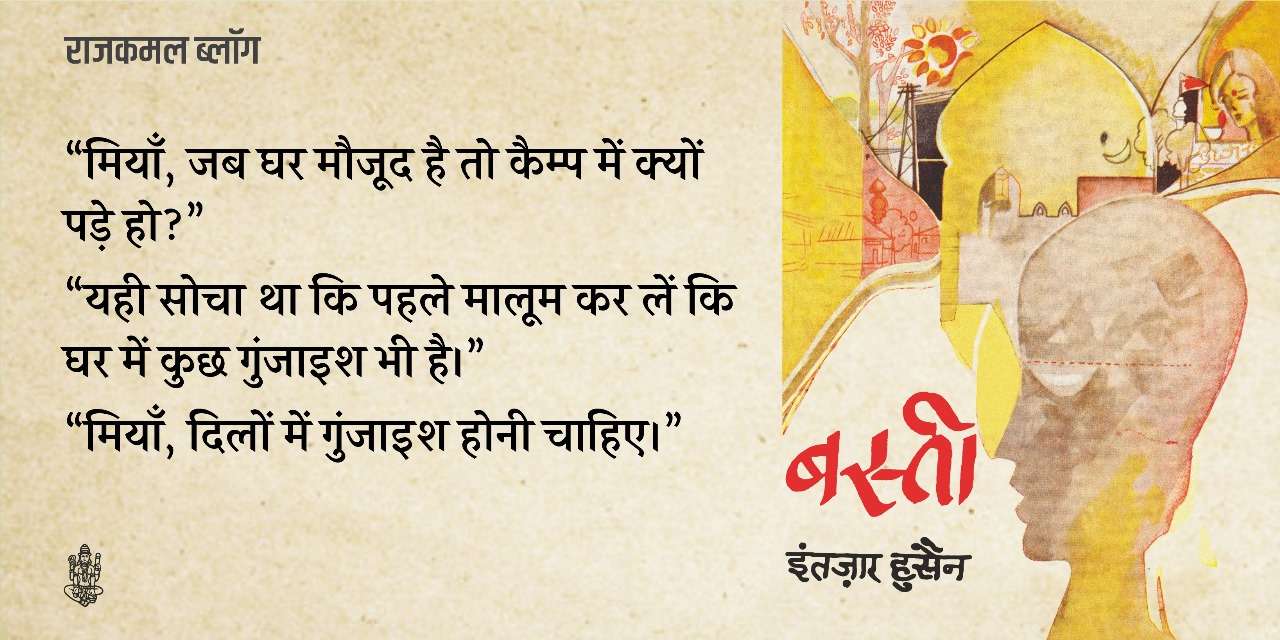वे दिन अच्छे ही थे― अच्छे और सच्चे। मुझे वे दिन याद रखने चाहिए, बल्कि लिख कर रख लेने चाहिए कि कहीं दिमाग़ से उतर न जाएँ। और बाद के दिन? उन्हें भी पता चले कि क्योंकर दिनों से अच्छाई और सच्चाई गुम होती चली गई, क्योंकर दिनों से ऊब और रातों से भय जुड़ता चला गया? किस तरह देखते-देखते शामनगर के मकान खुले से तंग होते चले गए और दिलों में गुंजाइश कम होती चली गई।
राजकमल ब्लॉग में आज पढ़ें, पाकिस्तान के शीर्षस्थ कथाकार इंतिजार हुसैन के उपन्यास ‘बस्ती’ का एक अंश। विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया यह उपन्यास मानवीय संवेदनाओं का एक महाआख्यान है। इस उपन्यास के लिए लेखक को पाकिस्तान के सबसे बड़े पुरस्कार ‘आदमजी एवार्ड’ से सम्मानित किया गया, जिसे उन्होंने वापस कर दिया।
...
कभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती। दरवाज़ा खुलने पर कभी सामान और सवारियों से लदा-फँदा ताँगा खड़ा नज़र आता, कभी अकेला आदमी, बेसरो-सामान, लिबास मैला-कुचैला, सिर में गर्द अटी हुई, शेव बढ़ी हुई। पहली नजर में सूरत पहचानने में न आती। जब पहचानी जाती तो आँखें हैरत से देखतीं, "अरे तुम हो!" एकदम गले लगाना, सवाल पर सवाल करना, "कैसे आए? रास्ते में खैरियत रही? बाक़ी लोग कहाँ हैं? क्या अकेले चले थे? सामान कहाँ है?"
"खैरियत कैसी? ट्रेन पर हमला हो गया था।"
"अल्लाह खैर करे, फिर?"
"बस अल्लाह ने खैर ही की। जान और आबरू रख ली, वरना कोई कसर तो नहीं रह गई थी।"
"अल्लाह तेरा शुक्र है! फिर बाक़ी लोग कहाँ हैं?"
"वालटन कैम्प में हैं।"
"मियाँ, जब घर मौजूद है तो कैम्प में क्यों पड़े हो?"
"यही सोचा था कि पहले मालूम कर लें कि घर में कुछ गुंजाइश भी है।"
"मियाँ, दिलों में गुंजाइश होनी चाहिए।"
गुंजाइश वैसे मकानों में भी कम नहीं थी। शामनगर में कितने मकान ख़ाली पड़े थे। कितने मकान थे कि खुले पड़े थे― दरवाजे और खिड़कियाँ सब खुले हुए, खुली खिड़कियों से घर में भरा साजोसामान नज़र आता हुआ। लगता था कि जाने वाले बस अचानक दामन झाड़कर उठ खड़े हुए और निकल गए। ऐसे भी मकान थे जिनमें मोटे-मोटे ताले पड़े थे। ऊपर-नीचे की सब खिड़कियाँ सावधानी से बन्द की हुई। लगता था कि जाने वाले वापसी के ख़याल से घरों को बन्द करके लम्बे सफ़र पर गए हैं। किसी-किसी घर की सबसे ऊपर की मंजिल की कोई खिड़की बेध्यानी में खुली रह गई थी और अब जब हवा तेज़ चलती थी तो खिड़कियाँ खुलतीं-बन्द होतीं, पट धाड़-धाड़ बोलते थे। कोई-कोई इमारत अधबनी पड़ी थी, कोई निर्माण के आखिरी दौर में आकर जहाँ की तहाँ रह गई थी। इन इमारतों वाले दूर के शहरों में सिर छुपाने के लिए कोने ढूँढ़ते फिरते होंगे। दूर के शहरों से आने वाले इन इमारतों में सिर छुपाने के लिए भाग-दौड़ करते फिरते थे। इन इमारतों में बहुत गुंजाइश थी। इन इमारतों से ज्यादा दिलों में गुंजाइश थी। हकीम बन्दे अली ने अपने क़ब्ज़े के दो-मंजिला मकान में कितने घरानों को पनाह दे रखी थी! ननवा उस वक़्त पहुँचा जब दोनों मंजिलें भर चुकी थीं।
"हकीम जी! मैं तो जी तुम्हारे इस बाहर के बरामदे में पड़ रहूँगा।"
"हाँ, हाँ, शौक़ से, हाज़िर में क्या हुज्जत है?"
ननवा ने अपने परिवार के साथ उस बाहर के बरामदे में डेरे डाल दिए। वे दिन अच्छे ही थे-अच्छे और सच्चे। मुझे वे दिन याद रखने चाहिए, बल्कि लिख कर रख लेने चाहिए कि कहीं दिमाग़ से उतर न जाएँ। और बाद के दिन? उन्हें भी कि पता चले कि क्योंकर दिनों से अच्छाई और सच्चाई गुम होती चली गई, क्योंकर दिनों से ऊब और रातों से भय जुड़ता चला गया? किस तरह देखते-देखते शामनगर के मकान खुले से तंग होते चले गए और दिलों में गुंजाइश कम होती चली गई। क़ाफ़िलों का ताँता टूट चुका था। बस कभी कोई इक्का-दुक्का आदमी, कभी कोई छोटा-मोटा ख़ानदान आ निकलता, शामनगर में भटकता फिरता। कहीं सिर छुपाने की जगह न मिलती।
शामनगर के सब मकान भर चुके थे, जो खुले पड़े थे वे भी, जो तालाबन्द थे वे भी, जो अधबने रह गए थे वे भी। जिस तालाबन्द इमारत के सबसे ऊपर के कमरे की खिड़की खुली रह गई थी और दोपहरों और रातों को तेज हवा चलने पर एक डरावने शोर के साथ खुलती और बन्द होती थी, अब उसके सदर दरवाज़े से बच्चे और जवान आते-जाते नज़र आते और उस खिड़की पर एक चिक पड़ी दिखाई देती थी। उससे ऊपरी मंज़िलों की खिड़कियों पर कहीं चिकें पड़ी थीं, कहीं रंगीन परदे, कहीं टाट। ऊँची मुंडेरों पर जो कल तक वीरान थीं, अब रंग- बिरंगे गीले कपड़े फैले नज़र आते। उस सफ़ेद अंडा-सी इमारत में, जिसके चौपट खुले दरवाजे अन्दर के फ़रनिश्ड कमरों का पता देते थे, अब उसके बाहर के चिप वाले बरामदे में भैंस बँधी नज़र आती थी और ड्राइंग रूम में नक़्शा यह दिखाई पड़ता था कि फ़रनीचर एक तरफ ढेर किया हुआ था, बाक़ी जगह में भूसे और उपले के ढेर।
शामनगर में अभावों का नक़्शा अब नहीं दिखता था। जिंदगी की जो जरूरतें सिमटते-सिमटते तन ढाँकने और पेट भरने तक सिमट गई थीं, अब फिर बढ़कर फैल गई थीं और बढ़ती-फैलती चली जा रही थीं। जिन मकानों ने कई-कई ख़ानदानों को पनाह दी, अब वे मकान बाक़ी खानदानों से खाली कराकर किसी एक खानदान के आवास थे। मगर इसके बावजूद अब उनमें मकानपन कम और उनमें रहनेवाले की जरूरतें ज्यादा नज़र आने लगी थीं। जिन मकानों में अभी तक अलग-अलग ख़ानदान हुँसे हुए थे, उनमें हर खानदान अपनी जिंदगी की ज़रूरतों में बढ़ोतरी करने के साथ-साथ फैलने की कोशिश कर रहा था। कोई-कोई मकान वाला फैलते-फैलते अपनी हदों से निकलकर दूसरे की हदों में फैलने पर उतारू नजर आता। दूसरी तरफ़ से विरोध होता। तू-तुकार, फिर एक का हाथ और दूसरे का गरीबान। लड़ने वाले पहले अन्दर-अन्दर लड़ते, फिर लड़ते-लड़ते बाहर निकल आते। पड़ोसी पहले तो तमाशा देखते। फिर बीच-बचाव करते। कोई फुर्तीला मकान वाला भाग-दौड़ करके पूरा मकान अपने नाम अलाट करा लेता। फिर उसमें बाक़ी रहने वाले टाँडा-बाँडा लादकर नए ठिकाने की तलाश में निकलते। जिसने निकलने से मना किया, वह थाने-कचहरी में खिंचा खिंचा फिरता।
"हकीम जी! क्या ननवा चला गया याँ से?" मैंने उस बरामदे को, जहाँ अब एक ठंडे चूल्हे के सिवाय कुछ नहीं रह गया था, हैरत से देखा और बग़ल के कमरे में जाकर जो हकीम बन्दे अली का दवाखाना था, सवाल किया।
"न जाता तो क्या करता ? पुलिस आकर बरतन-भाँडे सड़क पर फेंकने लगी थी।" वह चुप हुए, फिर बोले, "हम भी मकान की तलाश में हैं।"
"आप!"
"हाँ मियाँ, मैं। पुलिस के हाथों बेइज़्ज़त होने से यह कहीं अच्छा है कि आदमी ख़ुद ही उठ जाए।"
"मगर पहले तो आप ही इस मकान में आए थे, आप ही ने हम सब को पनाह दी थी।"
"बेटे! सोते की कटिया' जागते का कटरा। मुंशी मसीब हुसैन भागदौड़ करके अपने नाम का आर्डर ले आए हैं।"
वह रुके, फिर बोले, "उसकी आँख में सुअर का बाल है। वह किसी को यहाँ टिकने नहीं देगा।"
मैंने अन्दर जाकर जिक्र किया, "अब्बाजान! ननवा तो चला गया।"
अब्बाजान ने कोई जवाब नहीं दिया।
"और हकीमजी भी मकान की तलाश में हैं।"
अब्बा जान ने जैसे सुना ही नहीं।
"हाँ," अम्मी बोलीं, "तुम मकान कब तलाश करोगे?"
"हमें भी निकलना पड़ेगा?"
"क्यों तुम में क्या सुर्खाब के पर लगे हुए हैं।"
"अम्मी। यह मुंशी वहाँ तो ऐसा नहीं था।"
अम्मी ने ठंडी साँस भरी। "याँ आके तो लोगों की आँखों का पानी मर गया। तुझे तो क्या याद होगा, जब तेरे दादा अब्बा जिंदा थे तो यह मुंशी मुसीब हुसैन हमारी ड्योढ़ी नहीं छोड़ते थे। अल्लाह की शान कि अब हमें आँखें दिखाते हैं!"
अब्बाजान ने अम्मी को देखा, कुछ नाखुश-सी नज़रों से। फिर बोले, "वालिदे-मरहूम ने अपने वक़्त में किस-किसको फ़ायदा नहीं पहुँचाया, मगर किसी पर जताया नहीं।"
"हमने भी कब किसी पर जताया, मगर जब जी जलता है तो बात जुबान पर आ ही जाती है। वाँ पर क्या औक़ात थी! याँ आके गंजे को नाखून मिल गए।"
"ज़ाकिर की माँ, "अब्बाजान के लहजे में चेतावनी का रंग था, "अल्लाह-तआला घमंड करने वालों को पसन्द नहीं करता।"
"हाँ, मगर तुमने तो घमंड कभी नहीं किया था। ख़ुदा ने तुम्हें कितना पसन्द किया? आज सिर छुपाने के लिए कोई कोना नहीं है, "अम्मी ने जले-भुने लहजे में कहा और चुप हो गईं।
इंतज़ार हुसैन की पुस्तकें यहाँ से प्राप्त करें।