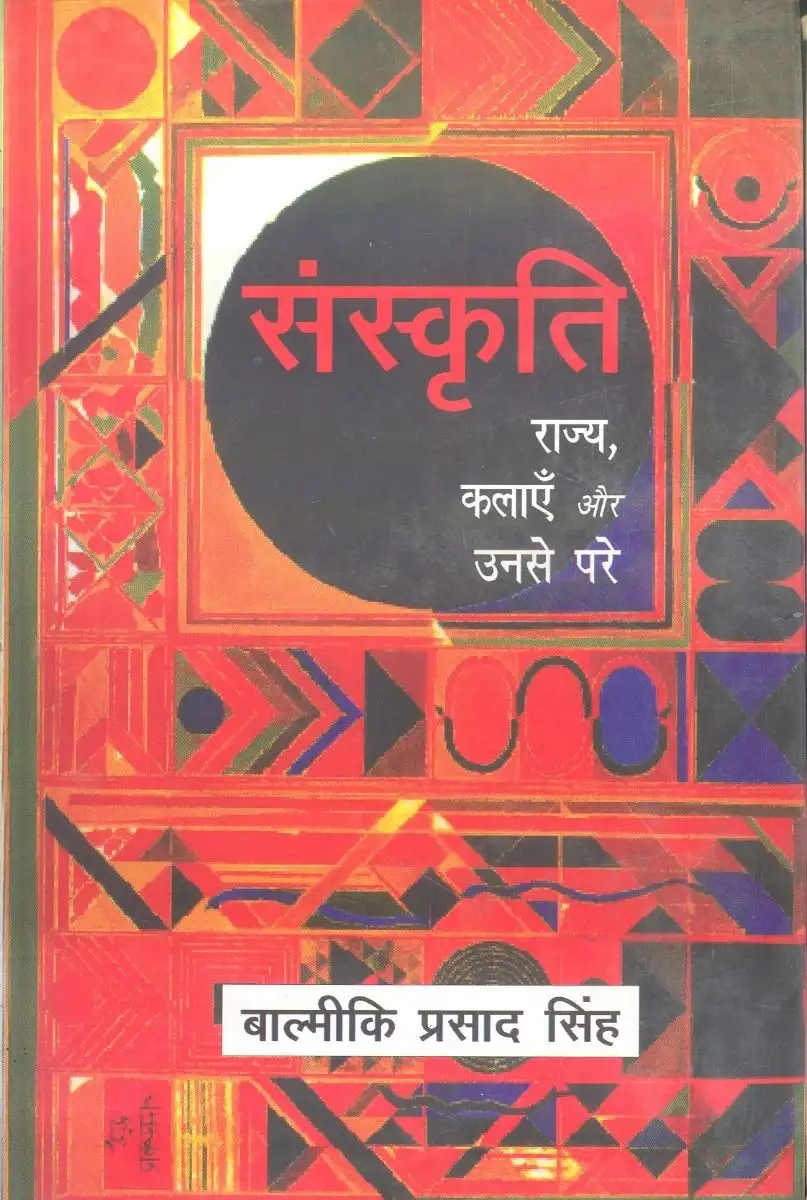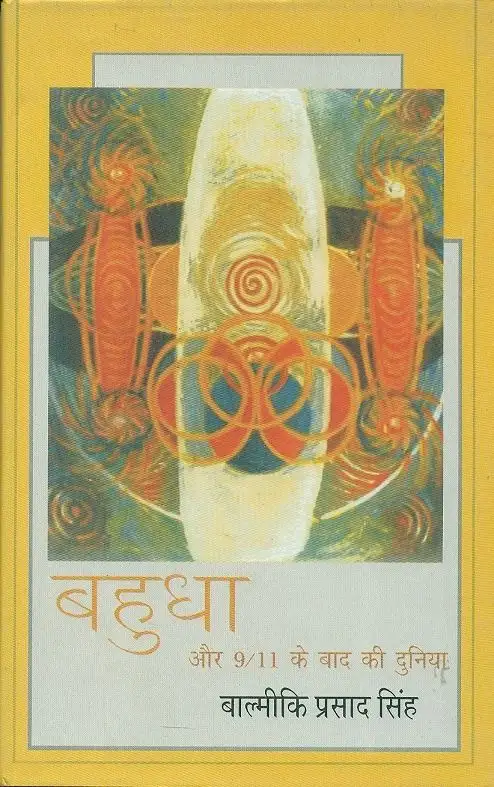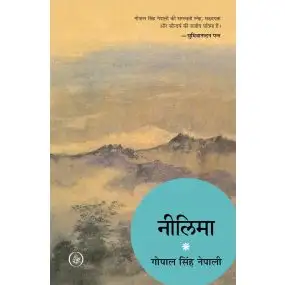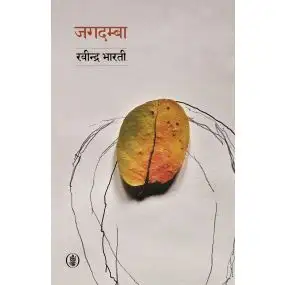संस्कृति भारतीय अनुभव की आत्मा है। भारतीय अनुभव को समझने के लिए आवश्यक है कि उसके मर्म में स्थित भारतीय संस्कृति को समझा जाए। ईसाई युग के अभ्युदय से काफ़ी पहले ही पूर्णत: विकसित हो चुकी इस संस्कृति ने भारतवासियों को (और समस्त भरतवंशियों को भी) एक निश्चित अस्मिता और चरित्र से सम्पन्न किया है। लेखक की मान्यता है कि संस्कृति के इसी अवदान के कारण भारतीय जन-गण इतिहास के कई दौरों और मानव-चेतना में हुए कई परिवर्तनों के बावजूद अपनी अखंडता सुरक्षित रख पाए हैं।
यह पुस्तक भारतीय संस्कृति की एक असाधारण अन्वेषण-यात्रा करते हुए व्याख्यात्मक प्रयास के ज़रिए कई अन्तर्सम्बन्धित विषय-वस्तुओं पर प्रकाश डालती है। इन्हीं में से एक धारणा यह है कि भारत में एक विकसित संस्कृति और विकासमान अर्थव्यवस्था का दुर्लभ संयोग मिलता है। लेखक का दावा है कि बीसवीं सदी के आख़िरी वर्षों में राष्ट्र-समुदाय के बीच राष्ट्रों की हैसियत तय करने में संस्कृति का कारक महत्त्वपूर्ण होता जा रहा है। शीतयुद्धोत्तर विश्व में ‘बाज़ार’ ने ‘सैन्य-शक्ति’ को प्रतिस्थापित कर दिया है और ‘संस्कृति’ अब इन दोनों के महत्त्व को चुनौती दे रही है। लेखक ने कला और संस्कृति के साथ भारतीय राज्य की अन्योन्यक्रिया की जाँच-पड़ताल ऐतिहासिक ही नहीं, समकालीन दृष्टिकोण से भी की है। उनकी मान्यता है कि जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद के ज़माने से ही भारत सरकार कला और संस्कृति के क्षेत्रों को प्रायोजित करने और संरक्षण देने की नीति के साथ प्रतिबद्ध रही है (इस विषय से जुड़े हुए कुछ पत्राचार सम्बन्धी अप्रकाशित दस्तावेज़ भी पुस्तक में उद्धृत किए गए हैं)।
नब्बे के दशक की शुरुआत से जारी अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और पश्चिमी मीडिया के प्रभावों के मद्देनज़र लेखक ने व्यापारिक क्षेत्र द्वारा संस्कृति के क्षेत्र में सरकार के साथ जुड़ने की आवश्यकता की ओर ध्यान खींचा है। उसका तर्क है कि धरोहर स्थलों के समुचित संरक्षण और भारतीय संस्कृति के रचनात्मक रखरखाव के लिए परियोजनाओं और कार्यक्रमों के प्रायोजित करने का दायित्व निभाने में निजी क्षेत्र सरकार की मदद कर सकता है। पुस्तक इस सम्बन्ध में विचारवान नागरिकों और स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका को उभारते हुए सुझाव देती है कि देश की सांस्कृतिक धरोहर के प्रबन्धन के लिए भारत सरकार को इस काम में विशेष रूप से पारंगत प्रशासनिक कैडर का गठन करना चाहिए। संस्कृति से सम्बन्धित यह सर्वथा नवीन विश्लेषण ‘सभ्यताओं में संघर्ष’ जैसी बहुप्रचारित धारणाओं को अस्वीकार करते हुए सभ्यताओं के बीच मैत्री का परिदृश्य व्याख्यायित करता है और उसे लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण के व्यापकतर सन्दर्भ से जोड़ देता है। लेखक की दलील है कि इस वैचारिक विन्यास के लिए आनेवाली सहस्राब्दि में गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी की शिक्षाएँ उत्तरोत्तर प्रासंगिक होती चली जाएँगी।
भारतीय सांस्कृतिक इतिहास, राजकीय नीति के विश्लेषण और दार्शनिक विचार-विमर्श के मिश्रण के माध्यम से यह पुस्तक राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर और उसके भारतीय व वैश्विक सन्दर्भों पर एक चुनौतीपूर्ण व नवीन दृष्टि डालती है।
| Language | Hindi |
|---|---|
| Binding | Hard Back |
| Translator | Not Selected |
| Editor | Not Selected |
| Publication Year | 1999 |
| Edition Year | 1999, Ed. 1st |
| Pages | 206p |
| Publisher | Rajkamal Prakashan |
| Dimensions | 22 X 14.5 X 1.5 |